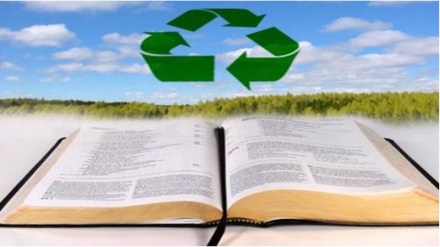हम और पर्यावरण-19
पर्यावरण के संबंध में पिछले कुछ दशकों से एक विषय जो बार बार चर्चा का केन्द्र रहा वह ग्रीन हाउस गैसों का विषय है।
इन गैसों को इसलिए ग्रीन हाउस कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन के परिवेश में ग्रीन हाउस जैसे वातावरण को जन्म देती हैं। ग्रीन हाउस में सूरज की किरण दाख़िल होती है लेकिन चूंकि उसकी दीवार शीशे की होती है इसलिए किरण का कुछ भाग ग्रीन हाउस में रह जाता है। इस प्रकार ग्रीन हाउस के भीतर का वातावरण बाहर के वातावरण से ज़्यादा गर्म होता है। ज़मीन के वायुमंडल में भी ऐसी ही घटना घटित होती है। सूरज की किरण जब ज़मीन पर पहुंचती है तो उसमें से कुछ ज़मीन अपने भीतर खींच लेती है जिससे ज़मीन की सतह गर्म हो जाती है। क्योंकि ज़मीन की सतह सूर्य की तुलना में बहुत ठंडी है। इसके नतीजे में सूर्य की किरणों की तुलना में लंबी वेवलेंथ का उत्सर्जन होता है। सूरज की किरणे ज़मीन से टकराने के बाद अधिक लंबी वेवलेंथ को उत्सर्जित करती हैं। दूसरी ओर ज़मीन का वायुमंडल लंबी वेवलेंथ को आसानी से अपने भीतर अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार ज़मीन से लौटने वाली वेव वायुमंडल में अवशोषित होकर वातावरण को गर्म कर देती है।
अलबत्ता यह प्रक्रिया अपने आप में ख़तरनाक नहीं है। प्रकृति में इंसान की गतिविधियों से होने वाले हस्तक्षेप से पहले ज़मीन का वायुमंडल सूरज की किरणों के एक भाग को अपने भीतर रोक लेता था जिसके नतीजे में ज़मीन पर जीवन के लिए उचित स्तर की गर्मी बनी रहती थी। ग्रीन हाउस गैसों के बिना धरती का तापमान लगभग 15-30 सेंटीग्रेड के बीच रहता था। लेकिन जबसे इंसानी गतिविधियां बढ़ीं तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा जिससे सूरज की किरणों का अवशोषण बढ़ गया। औद्योगिक क्रान्ति शुरु होने और जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बढ़ने से पर्यावरण में गैसों का काम्पज़िशन बदल गया है और सूरज की किरणों के अवशोषण का स्तर बढ़ गया है।
लगभग सभी लोग जो ग्रीन हाउस गैसों की शब्दावली से परिचित हैं वे कार्बन डायऑक्साइड को इस समूह का परिचय कराने वाली गैस के रूप में जानते हैं। जबकि यह इस समूह की एक गैस है। ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प, कार्बन डायऑक्साइड, नाइट्रोजन डायऑक्साइड, मिथेन और ओज़ोन गैस हैं। जलवाष्प, कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन और ओज़ोन ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा प्रभावी गैस हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में इनमें से हर एक गैसों की सटीक मात्रा का निर्धारण मुमकिन नहीं है लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक़ जलवाष्प की 36 से 70 फ़ीसद, कार्बन डायऑक्साइड की 9 से 26 फ़ीसद, मिथेन की 4 से 9 फ़ीसद और ओज़ोन की लगभग 3 से 7 फ़ीसद भागीदारी होती है। पर्यावरण के मुख्य अंश अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सिजन ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं हैं क्योंकि इनके दोनों मोलेक्यूल इन्फ़्रारेड रेडिएशन अर्थात अवरक्त विकिरण को न तो अवशोषित और न ही प्रतिबिंबित करते हैं जिसके नतीजे में इनके मोलेक्यूल में कोम बदलाव नहीं आता। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा चिंता कार्बन गैसों को लेकर है जो मानव गतिविधियों से वजूद में आती हैं। पर्यावरण में कार्बन गैस का घनत्व औद्योगिक क्रान्ति के शुरु में लगभग 280 यूनिट थी जो इस वक़्त बढ़कर 350 यूनिट हो गयी है और इस बात का डर है कि अगर यह प्रक्रिया यूहीं जारी रही तो 2050 तक यह यूनिट 450 तक पहुंच जाएगी।
जब बात ग्रीन हाउस गैसों की होती है तो इससे आशाय पर्यावरण पर इन गैसों का पड़ने वाले प्रभाव होता है। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में जीन फ़ूरियर ने ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के बारे में बताया। ग्रीन हाउस गैस के असर का अर्थ है धरती के वायुमंडल का गर्म होना है। सूरज की किरणों के इन गैसों के बीच से गुज़रकर ज़मीन में अवशोषित होने या वायुमंडल में पलटने के नतीजे में वायुमंडल गर्म हो जाता है।
ज़्यादातर मानव गतिविधियों के नतीजे में ग्रीन हाउस गैस पैदा होती हैं। औद्योगिक क्रान्ति और औद्योगिक उपकरणों के आविष्कार के बाद, इंसान ने कृषि और औद्योगिक गतिविधियों से ज़मीन, पानी और हवा का काम्पज़िशन बदल गया। औद्योगिक क्रान्ति से इंसान की जीवन शैली बदल गयी। बढ़ती आबादी और तेल व पत्थर के कोयले के बढ़ते इस्तेमाल से वायमुंडल में गैसों का काम्पज़िशन भी बदल गया। शोध के अनुसार, हर साल जीवश्म ईंधन से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ से वायुमंडल में हर साल 25 अरब टन कार्बन डायऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन ओईसीडी के सदस्यों देशों में हुए अध्ययन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि 40 से 50 फ़ीसद सल्फ़र डायऑक्साइड, 25 फ़ीसद नाइट्रोजन डायऑक्साइड और 50 फ़ीसद से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों में ख़ास तौर पर कार्बन गैस थर्मल पावर स्टेशन से उत्सर्जित होती हैं। फ़सल की कटाई के बाद खेतों में मौजूद अवशेष को जलाने से कार्बन डायऑक्साइड का उत्पादन होता है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव तेज़ हो जाता है और फ़ूड चेन में मौजूद कार्बन इन चेनों से निकल जाता है और फिर दुबारा उसमे दाख़िल नहीं होता कि इसका पर्यावरण और इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ता है।
ग्रीन हाउस गैस का एक स्पष्ट असर धरती का बढ़ता तापमान है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि पिछले 100 साल में धरती का तापमान अवसतन 0.18 से 0.74 सेंटीग्रेड तक बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन के बारे में सबसे प्रतिष्ठित संस्था आईपीसीसी ने भी एक रिपोर्ट में इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा है कि बीसवीं शताब्दी के बीच में बढ़ते तापमान का बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन था जो इंसानी गतिविधियों से पैदा होती हैं। आईपीसीसी के जलवायु परिवर्तन से संबंधित मॉडल दर्शाता है कि अगर यह प्रक्रिया इसी तरह जारी रही तो 1990 से 2100 के बीच धरती के तापमान में 1.1 से 4.6 सेंटीग्रेड बीच अतिरिक्त तापमान की वृद्धि हो जाएगी।
इसी प्रकार वैज्ञानिक शोध दर्शाता है कि अगर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ख़ास तौर पर कार्बन गैस का उत्सर्जन इसी रफ़्तार से तरह जारी रहा मौजूदा दौर में जारी है तो 2030 तक धरती के तापमान में अवसतन 1 से 2 सेंट्रीग्रेड वृद्धि हो जाएगी। बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवीय इलाक़ों में बहुत बदलाव आएगा क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवीय इलाक़ों की बर्फ़ पिघलेगी जिससे महासागरों, तटवर्ती इलाक़ों का जलस्तर बढ़ेगा जिसके नतीजे में बड़ी मात्रा में खेती की ज़मीनें पानी में डूब जाएंगी। इसी प्रकार इस बात का अनुमान है कि भारत, बांग्लादेश और यूरोप के कुछ तटवर्ती शहरों के पानी में डूबने का ख़तरा है। यूरोन्यूज़ चैनल ने एक रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते उत्सर्जन का उल्लेख करते हुए सचेत किया है कि अगर उत्सर्जन की मौजूदा प्रक्रिया इसी प्रकार जारी रही तो 2080 तक दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा लोग पानी की कमी की समस्या का सामना करेंगे और समुद्र का जलस्तर 60 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा।
वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आज से हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोक दें तब भी अगले बीस साल में 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। यद्यपि तापमान बढ़ने की यह मात्रा बहुत अधिक नहीं लग रही है लेकिन लंबे समय में वायुमंडल में बहुत गंभीर परिवर्तन ला सकती है जिससे बारिश का स्तर बदल जाएगा और बहुत ही विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। इस बदलाव के नतीजे में बाढ़ और तूफ़ान जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। इसी प्रकार धरती के बढ़ते तापमान से साल में गर्मी के दिन बढ़ जाएंगे जिसके नतीजे में लू लगने और मलेरिया की समस्या जन्म लेगी। आम तौर पर निर्धन देशों में बच्चे और बूढ़े इसकी भेंट ज़्यादा चढ़ेंगे। बढ़ते तापमान से इंसान के सामने मीठे पानी की समस्या सिर उठाएगी। इस बदलाव का पशुओं और वनस्पतियों पर भी नकारात्म असर पड़ेगा। ख़ास तौर पर अगर यह बदलाव तेज़ी से हुआ तो जंगली जानवरों के जीवन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर साल की विभिन्न फ़सलों में पलायन करने वाले पक्षियों के लिए पलायन करने के लिए उचित स्थल नहीं रहेगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ की ताज़ा रिपोर्ट दर्शाती है कि दुनिया में ग्रीन हाउस गैस का 70 फ़ीसद उत्सर्जन औद्योगिक देश करते हैं। इस रिपोर्ट में इसी प्रकार इस बात का भी उल्लेख है कि इंसानी गतिविधियों से पैदा होने वाले कार्बन की मात्रा इस समय 36 गीगाटन है जिसकी मात्रा 2050 तक घट कर 11 गीगाटन होनी चाहिए।