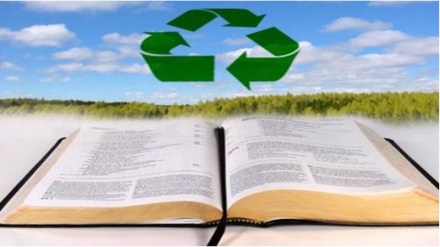हम और पर्यावरण-20
औद्योगिक क्रांति के बाद से कि जो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग की शुरूआत का भी समय था आज तक, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग में इंसान की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है।
मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि आज जिस चीज़ का भी हम उत्पादन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसे फेंक देते हैं, इसका अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। विश्व स्रोत संस्था और अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन समिति के आंकड़ों के अनुसार, इंसानी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का एक मुख्य कारण, ऊर्जा संयंत्र हैं, यह इस प्रकार की गैसों के उत्सर्जन का सबसे मुख्य एवं प्रभावशाली कारण है। विश्व में अनेक ऊर्जा संयंत्रों का संचालन नेच्यूरल गैस, कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों से होता है, जो सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं।
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जंगलों का विनाश है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जंगलों के विनाश की भागीदारी 20 प्रतिशत है। जंगलों के विनाश से न केवल कार्बन डाइआक्साइड के जज़्ब होने की क्षमता कम हो जाती है, बल्कि पेड़ों में एकट्ठा होने वाला कॉर्बन और मीथेन भी हवा में शामिल हो जाता है। इसका एक अन्य कारण, सड़कों पर चलने वाला ट्रैफ़िक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इसका हिस्सा 13 प्रतिशत है। यात्री विमानों से हर प्रति किलोमीटर केवल 5 फ़ीसद कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन यह मात्रा ट्रेनों से 3 गुना अधिक है।
तेल और गैस के उत्पादन से कार्बन डाइआक्साइड और मीथेन गैसों के उत्सर्जन के अलावा 6 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तेल और गैस के निकालने और उसके रिफ़ाइनमैंट में काफ़ी अधिक ऊर्जा के इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा, इससे ज़मीन के अन्दर से मीथेन गैस निकलकर वातावरण में फैल जाती है। मीथेन गैस में कार्बन डाइआक्साइड की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक ऊष्मा होती है।
कृषि गतिविधियां भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रभावी हैं। कैमिकल खाद से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन होता है, जिससे दुनिया में 6 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। आधुनिक कृषि काफ़ी हद तक कैमिलकल खादों और कीटनाशकों पर निर्भर करती है, जिसका उत्पादन कच्चे तेल और गैसों से होता है। इन उत्पादों के इस्तेमाल से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से निकलने वाली गर्मी कार्बन डाइआक्साइड से 300 गुना अधिक होती है।
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में पशुपालन की भागीदारी 5 प्रतिशत है। विश्व में मीथेन गैस के उत्सर्जन में पशुपालन की भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत है। सीमेंट उद्योग, उड्डयन उद्योग, स्पात और कूड़े से भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। यहां सवाल यह है कि कौन से देश सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं।
2007 में राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में सबसे अधिक अमरीका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़ चीन ने अब अमरीका का स्थान ले लिया है। चीन तेज़ी से विकास के कारण दुनिया में 25 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। लेकिन इस स्थानांतरण में एक ध्यान योग्य बिंदु भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक़, चीन में अधिक मात्रा में स्पात का उत्पादन होता है, लेकिन अंततः इसे अमरीका निर्यात कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप, इस उत्पादन में चीन की भागीदारी हवा को प्रदूषित करने में है, जबकि इसकी डिमांड अमरीका में है। इसके बावजूद कि इस उत्पाद का उपभोग कहां होता है बजाए इसके कि इसका उत्पादन कहां होता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन करने वाले देशों की सूचि में चीन सबसे ऊपर है, हालांकि उसके और अमरीका के बीच अधिक फ़ासला नहीं है। इस आधार पर कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में चीन की भागीदारी 21.9 प्रतिशत और अमरीका की 18.1 प्रतिशत है। इस संदर्भ में एसोशिएट्ड प्रेस ने लिखा है, चीन और अमरीका के बाद भारत, 6.6, रूस 5.1 और जापान 3.7 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं।
पर्यावरण के विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद, दिसम्बर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रहण किया गया, इसमें 160 देश ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हुए। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार, विश्व के 36 औद्योगिक देशों की ज़िम्मेदारी थी कि 1990 की तुलना में 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में औसतन 5 प्रतिशत की कमी करें, लेकिन यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इसलिए कि अमरीका एकमात्र ऐसा देश था, जिसने वर्षों तक क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया था। अमरीकी अधिकारियों का मानना था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के कारण, आर्थिक प्रगति में कमी हो सकती है और इस प्रकार अमरीका अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा। उस समय तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने तर्क दिया था कि क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार करने से अमरीका को 400 अरब डॉलर का नुक़सान होगा और 50 लाख लोग बेरोज़गार हो जायेंगे।
इस संधि पर हस्ताक्षर न करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने अमरीका की आलोचना की और जी-8 देशों के सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित वार्ता में अमरीका अलग थलग पड़ गया। हालांकि अमरीका ने 2006 में एशिया और प्रशांत माहासागर क्षेत्र में स्वच्छ हवा और पानी के विषय पर बैठक का आयोजन करके इस स्थिति से निकलने की कोशिश की। इस बैठक में चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत ने भाग लिया। लेकिन इस संधि की इसलिए आलोचना हुई, क्योंकि इसका सदस्य बनने के लिए कोई भी देश पर्यावरण से संबंधित विषयों के लिए प्रतिबद्ध नहीं था।
इस संदर्भ में अमरीका के पूर्व उप राष्ट्रपति अलगोर और जलवायु की सुरक्षा के लिए गठजोड़ के अध्यक्ष ने कहा था कि अमरीका में क्योटो प्रोटोकॉल की इतनी बुराई हुई है कि मैं नहीं समझता हूं कि इसे यहां स्वीकृति मिलेगी। यहां तक कि अमरीका में होने वाले सर्वों से पता चलता था कि अधिकांश लोगों का मानना है कि राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन की जो ख़राब स्थिति पेश कर रहा है, स्थिति उतनी ख़राब नहीं है। इस प्रकार की नीतियों के कारण, अमरीका न केवल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने में सफल नहीं हुआ, बल्कि आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक़ इस दौरान, इस देश में इन गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। यह ऐसी स्थिति में है कि जब अनेक वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 5 प्रतिशत की कटौती को अपर्याप्त माना है और उनका मानना है कि पर्यावरण को सही रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कम से कम 60 प्रतिशत की कटौती होनी चाहिए।
पर्यावरण की संकटमय स्थिति के दृष्टिगत 2007 में इंडोनेशिया के बाली में एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के लिए 10 हज़ार प्रतिनिधि शामिल हुए। यह ऐसा समझौता था जिसे क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर रहने वाले अमरीका और चीन ने भी स्वीकार कर लिया। इस बैठक की एक बड़ी चुनौती विकसित एवं विकासशील देशों के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन का न्यायपूर्ण बंटवारा करना था। बाली सम्मेलन में अमरीकी अधिकारियों की प्रतिक्रिया बहुत आश्चर्यजनक थी। इसलिए कि उन्होंने शुरू में बल देकर कहा कि वे क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस हस्ताक्षर के लिए सहमति दे दी। विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपीय संघ द्वारा इस समझौते के समर्थन के बाद अमरीका इसके विरोध में अकेला पड़ गया, इसलिए उसने ने भी सहमति का एलान कर दिया।
यूरोपीय देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 25 से 40 प्रतिशत की कटौती की मांग कर रहे थे। लेकिन अमरीकी प्रतिनिधिमंडल ने बाली सम्मेलन में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कमी के लिए मात्रा के निर्धारण और उसके पालन को अनिवार्य बनाने का विरोध किया, अंत में यूरोपीय देशों ने भी अमरीका की इस मांग का समर्थन कर दिया। पर्यावरण का समर्थन करने वाले संगठनों ने इस क़दम का कड़ा विरोध किया, जिसे अमरीका के आग्रह के कारण स्वीकार किया गया था।
हालांकि समय बीतने के साथ और अमरीकी जनता पर ग्रीन हाउस गैसों के पड़ने वाले प्रभावों के अधिक स्पष्ट होने के बाद, बराक ओबामा ने स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण को कम करने की नीति अपनाई। अमरीकी डेमोक्रेट इस नतीजे पर पहुंचे कि आने वाले समय में प्रदूषण के प्रभावों से बचने पर होने वाला ख़र्च वर्तमान में होने वाले आर्थिक लाभ से कहीं अधिक होगा। इसके अलावा, जलवायु से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौतों को स्वीकार करने के लिए वाशिंग्टन पर विश्व समुदाय के अधिक दबाव के कारण, अमरीका इसका विरोध नहीं कर सकता। यही कारण है कि उसने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के प्रोटोकॉल को स्वीकार किया है।
इसके बावजूद, अमरीकी सरकार की सहमति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन के बीच काफ़ी फ़ासला है। अमरीका में उद्योग और व्यापार निजी कंपनियों के हाथों में है, इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि निवेशक एवं पूंजीपति आसानी से पर्यावरण के पुनर्निमाण पर भारी ख़र्च के लिए राज़ी होंगे। अमरीका में तेल एवं ऑटोमोबाइल कंपनियों का काफ़ी प्रभाव है। यह कंपनियां सरकार के निर्णयों के सामने डट सकती हैं। इसलिए इस बात का संदेह है कि अमरीकी सरकार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की अपनी प्रतिबद्धता का पालन कर पाएगी।