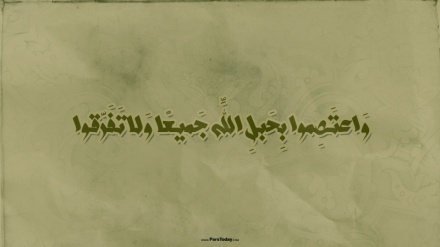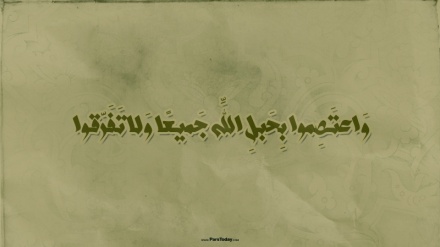इस्लामी जगत-8
आपको याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने इस बात का उल्लेख किया कि अल्लामा इक़बाल का मानना था कि इस्लामी जगत में पिछड़ेपन व पतन का कारण इस्लामी मूल्यों से दूरी है इसलिए वह इस्लामी जगत का अपनी संस्कृति व सभ्यता की ओर लौटने का आह्वान करते थे।
अल्लामा इक़बाल के ज़माने में ज़्यादातर बुद्धिजीवियों का ध्यान पश्चिमी विचारों को ओर था लेकिन अल्लामा इक़बाल पश्चिमी विचारों की आलोचना करते और इस बिन्दु पर बल देते थे कि मुसलमानों को चाहिए कि अपनी इस्लामी पहचान व एकता को फिर से हासिल करें। उन्होंने इस्लामी जगत में एकता के लिए चार सिद्धांतों पर आधारित इस्लामी आंदोलन का विचार पेश किया। वह चार सिद्धांत इस प्रकार हैं, पहला पवित्र क़ुरआन पर आस्था और उसका पालन, दूसरा इस्लामी परंपराओं की ओर लौटना, तीसरे इस्लामी शरीआ का पालन और चौथे एक राष्ट्रीय केन्द्र का गठन।
शैख़ मोहम्मद अब्दोह और रशीद रज़ा उन मुसलमान विचारकों में हैं जिन्होंने इस्लामी जगत में एकता के विचार को फैलाने की कोशिश की। शैख़ मोहम्मद अब्दोह मिस्र के उन प्रभावशाली विचारकों में हैं जिन पर सय्यद जमालुद्दीन असदाबादी के विचारों का प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस्लामी जगत में एकता के विचार को फैलाने की कोशिश की। शैख़ मोहम्मद अब्दोह ने कि जिन्हें सय्यद जमाल के शिष्यों में गिना जाता है, धार्मिक विचार को फैलाने की कोशिश की। इसी प्रकार उन्होंने इस्लाम की नई व्याख्या के ज़रिए समय के तक़ाज़ों के अनुसार, मुसलमानों की ज़रूरतों के पूरा करने की कोशिश की। सय्यद जमाल इस्लामी जगत में एकता और वैचारिक व राजनैतिक सुधार के लिए इस्लामी शासन के गठन को ज़रूरी समझते थे, जबकि शैख़ अब्दोह ने इस्लामी जगत में एकता के मार्ग में मुख्य रुकावट साम्राज्य से संघर्ष को प्राथमिकता देने के बजाए मुसलमानों में वैचारिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक सुधार को अपने कार्यक्रम में प्राथमिकता दी।
शैख़ मोहम्मद अब्दोह भी सय्यद जमाल की तरह यह मानते थे कि इस्लामी जगत में फूट का मुख्य कारण मुसलमानों में शिया-सुन्नी के बीच धार्मिक मतभेद है। उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की किताब नहजुल बलाग़ा की एक व्याख्या लिखकर शिया-सुन्नी के बीच मतभेद को हल करने की कोशिश की। शैख़ मोहम्मद अब्दोह इस्लामी जगत में एकता के लिए तीन उसूलों पर बल देते थे, पहला यह कि इस्लाम में धर्म और बुद्धि के बीच संतुलन ज़रूरी है, दूसरे यह कि एकेश्वरवाद, बौद्धिक आधार, और समय के तक़ाज़ो को ध्यान में रखते हुए इज्तेहाद ज़रूरी है और तीसरे यह कि ज़िम्मेदारी के साथ इंसान के संकल्प और आज़ादी के बीच संपर्क है। इस्लामी जगत में पवित्र क़ुरआन, पैग़म्बरे इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों के कथन, विवेक और धर्म गुरुओं की सर्वसम्मति के आधार पर फ़त्वा देने की योग्यता को इज्तेहाद कहते हैं। शैख़ मोहम्मद अब्दोह ने ऐसे हालात में कि जब 19वीं शताब्दी में इस्लामी देशों में यूरोप के सांस्कृतिक प्रभाव और सत्ता के विस्तार ने भीतरी भ्रष्टाचार और विदेशी ख़तरों से निपटने के लिए एक इस्लामी आंदोलन की पृष्ठिभूमि मुहैया की थी, इस बात की कोशिश की कि पश्चिमी विचारों के ज़रिए इस्लामी जगत में बदलाव लाएं। उन्होंने मिस्र में इस्लामी सुधार आंदोलन चलाया कि जो दो जंगों के बीच के वर्षों में अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व वैचारिक दबाव का केन्द्र समझा जाता था।
इस्लामी जगत में एकता के लिए धार्मिक विचारों को जीवित करने की प्रक्रिया को शैख़ मोहम्मद अब्दोह के सीरियाई शिष्य रशीद रज़ा ने आगे बढ़ाया। वह सीरिया के उन शरणार्थियों में थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मिस्र को अपने वैचारिक व सांस्कृतिक गतिविधियों एवं वतन के रूप में चुना। रशीद रज़ा जातीय भेदभाव की भर्त्सना करते थे। वह राष्ट्रवाद के आलोचक होने के बावजूद सीरियाई अरब राष्ट्रवाद के सक्रिय प्रवक्ता थे। वह 1920 में सीरिया की राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष बने और फ़ैसल को सीरिया का शासक नियुक्त किया। रशीद रज़ा के विचार अरब राष्ट्रवाद की शिक्षाओं व भावनाओं तथा इस्लामी विश्वव्यापकता के विचार का संगम थे। रशीद रज़ा जो नारे और सुधारवाद के सिद्धांत की नज़र से सय्यद जमाल और शैख़ मोहम्मद अब्दोह का अनुसरण करते थे, अपने उस्ताद शैख़ अब्दोह के विपरीत ख़िलाफ़त के बाक़ी रहने पर बहुत बल देते थे। वह तत्कालीन ख़िलाफ़त में सुधार और उसे इस्लामी जगत के आरंभिक दौर की ख़िलाफ़त का रूप देने पर बल देते थे। रशीद रज़ा ने अपने जीवन काल में ख़िलाफ़त के संकट को दूर करने की कोशिश की। उनका मानना था कि तुर्कों की ख़िलाफ़त इस्लाम के न्यायवादी सिद्धांतों से दूर हो गयी है। वह ख़िलाफ़त को इस्लामी शिक्षाओं का ज्ञान रखने वालों, कि जिन्हें अहले हल्लो अक़्द कहा जाता है, की शैली द्वारा स्थानांतरित किए जाने के समर्थक थे। अहले हल्लो अक़्द उन्हें कहा जाता है जो धर्म का ज्ञान रखने के साथ साथ जनता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।
रशीद रज़ा के किसी ख़लीफ़ा या ख़िलाफ़त के लिए किसी विशेष शहर पर बल न देने के पीछे शायद राजनैतिक कारण भी हो सकता है क्योंकि उस समय ख़िलाफ़त के लिए सबसे बड़े दावेदार समझे जाने वाले उम्मीदवार अर्थात शरीफ़ हुसैन पर रशीद रज़ा को भरोसा नहीं था क्योंकि शरीफ़ हुसैन का व्यवहार अत्याचारपूर्ण था, उनमें धार्मिक समझ का अभाव था, वे ब्रिटेन के समर्थक थे और सुधारवादी प्रक्रिया के ख़िलाफ़ थे। इसी प्रकार उन्हें इस बात पर भी गहरा संदेह था कि किसी शिया ख़लीफ़ा को सुन्नी स्वीकार करेंगे यही कारण है कि उन्होंने इस विषय को उठाया कि ख़िलाफ़त के लिए आदर्श शर्तों को पूरा करने वाला कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है और स्थान की दृष्टि से हेजाज़ (वर्तमान सऊदी अरब) और इस्तांबोल उचित स्थान नहीं हैं इसलिए उन्होंने यह विचार पेश किया कि ख़िलाफ़त को तुर्कों और अरब प्रायद्वीप के अरबों के बीच सहयोग से दुबारा वजूद दिया जाए।
रशीद रज़ा इस वास्तविकता को भी स्वीकार करते हैं कि अरब और तुर्क विकास के उस चरण तक नहीं पहुंचे हैं कि इस संदर्भ में ज़रूरी सहयोग करें इसलिए वह यह सुझाव पेश करते हैं कि ख़िलाफ़त को अरब प्रायद्वीप और अनातोली के बीच में स्थित क्षेत्र में क़ायम किया जाए कि जहां अरब, तुर्क और कुर्द एक साथ ज़िन्दगी गुज़ारते हैं। उन्होंने साफ़ तौर पर मूसिल का नाम लिया था और उम्मीद जतायी थी कि जब यह इलाक़ा ख़िलाफ़त का केन्द्र घोषित होगा तो ये देश इस विषय पर विवाद खड़ा नहीं करेंगे और मूसिल जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आध्यात्मिक संबंध व शांति को जोड़ने वाला स्थान बन जाएगा। रशीद रज़ा के इस्लामी जगत में एकता से संबंधित विचार और सय्यद जमाल व मोहम्मद अब्दोह जैसे समाज सुधारकों के विचारों में बहुत से समान बिन्दु हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ख़िलाफ़त व इस्लामी हुकूमत की मूल व्यवस्था के दूसरी स्वाधीन इस्लामी सरकारों के साथ संबंध के बारे में नए विचार पेश किए थे।
रशीद रज़ा ने इस्लामी जगत में एकता व एक व्यवस्था क़ायम करने के लिए यह सुझाव पेश किया कि मौजूदा दौर के मुसलमान राष्ट्रों के अनुकूल नियम बनाए जाएं। वह इन नियमों के संकलन के लिए विभिन्न इस्लामी क्षेत्रों के योग्य लोगों से विचार विमर्श को ज़रूरी मानते थे और उनका मानना था कि ये योग्य लोग चार इस्लामी मतों के इस्लामी आदेश को पवित्र क़ुरआन और पैग़म्बरे इस्लाम की परंपरा से अनुरूपता दें और नियमों की ऐसी किताब संकलित करें जो ईश्वरीय क़ानून पर आधारित हो और जन हित के पालन, मुसलमानों के कल्याण और मौजूदा दौर की ज़रूरतों को पूरी करने से संबंधित दूसरे नियमों पर बाद में ध्यान दें। रशीद रज़ा का मानना था कि इन नियमों के संकलन के बाद ख़लीफ़ा उन्हें लागू कराए और इस्लामी देशों में दूसरे ख़लीफ़ाओं को इन नियमों को लागू करने का आदेश दे और नियमों के क्रियान्वयन पर नज़र रखे। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि इस्लामी जगत में एकता व सहयोग, मुसलमानों और इस्लामी देशों में जागरुकता पैदा करना ही रशीद रज़ा की कोशिशों का केन्द्र बिन्दु था। इस संदर्भ में उनकी कोशिशें तीन तरीक़ों से सामने आयीं। पहला तरीक़ा यह था कि ‘अलमनार’ पत्रिका में उनका लेख छपता और इसी प्रकार पूरी दुनिया में इस्लामी मतों को एक दूसरे के निकट लाने और इस्लामी जगत में एकता से संबंधित होने वाले प्रयास की ख़बरों को छापते थे। दूसरा तरीक़ा यह था कि वह शिक्षा केन्द्रों और इस्लामी हल्क़ों में भाषण देते थे और तीसरा यह था कि उन्होंने अलवहदतुल इस्लामिया जैसी किताब लिखी। रशीद रज़ा के मसुलमानों को एक दूसरे के निकट लाने के लिए ‘अलमनार’ पत्रिका में बहुत से लेख छपे। वह इस्लामी जगत के धर्मगुरुओं को आमंत्रित करते थे ताकि वे इस्लामी जगत में एकता के लिए अपने दृष्टिकोण पेश करें और मुसलमान भी इस आह्वान के नतीजे में अपनी समस्याओं को धार्मिक मामलों को बयान करते थे जैसा कि मोरक्को और ट्यूनीशिया से लेकर भारत और इंडोनेशिया तक यह संपर्क व सहयोग ‘अलमनार’ पत्रिका के ज़रिए क़ायम हुआ था।
रशीद रज़ा ज़ायोनीवाद और साम्राज्यवादियों की ओर से ख़तरों से मुसलमानों व अरबों को सचेत करते रहते थे। इसी प्रकार व ज़ायोनीवाद और साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ इस्लामी एकता पर आग्रह करते थे। रशीद रज़ा इसी प्रकार ‘अलमनार’ पत्रिका में उन विचारों की समीक्षा करते थे और उन्हें इस्लामी जगत की वैचारिक व्यवस्था में दाख़िल होने से रोकते थे जिन्हें इस्राइलियात कहा जाता है कि इस्राइलियत का लक्ष्य इस्लामी जगत में फूट डालना है। उनका मानना था कि मुसलमानों में पिछड़ापन उसी वक़्त दूर होगा जब इस्लामी जगत में एकता होगी और धार्मिक मतों में आपस में एक दूसरे से निकटता हो।