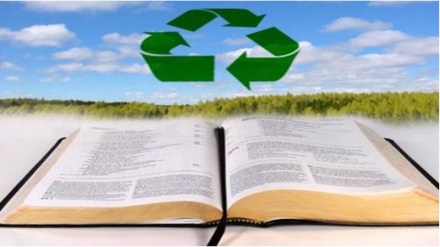हम और पर्यावरण-31
विशेषज्ञों के अनुसार पर्यावरण को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नुक़सान पहुंचाने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक विश्व स्तर पर और विशेष रूप से विकासशील देशों में आबादी का लगातार बढ़ना है।
आंकड़ों से पता चलता है कि हर चार दिन में दुनिया की आबादी में दस लाख लोगों की वृद्धि हो जाती है। यह संख्या पहली नज़र में तो बहुत अधिक नहीं लगती लेकिन कुछ ही साल में देखने में यह आता है कि दुनिया की जनसंख्या दुगनी हो गई और इसके साथ ही अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जनसंख्या में वृद्धि पर्यावरण संबंधी सभी समस्याओं की जटिलता बढ़ने का कारण है। वर्ष 2000 में ब्राउन और नेल्सन के अध्ययन से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई। यह दोनों शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि जनसंख्या में वृद्धि से धरती, पानी और वायु मंडल पर पड़ने वाला प्रदूषण का दबाव बढ़ जाता है।
जब दुनिया की आबादी बढ़ती है तो भूमिगत संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ता है क्योंकि जनसंख्या का खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि से सीधा संबंध है और इस अधिक खाद्य पदार्थ के उत्पादन के लिए अधिक संसाधन प्रयोग होते हैं तथा मांसाहार तैयार करने के लिए अधिक जानवरों का प्रयोग होता है। इस समय दुनिया की लगभग 50 प्रतिशत बायोलोजिकल विविधताएं इंसानों द्वारा प्रयोग कर ली जाती हैं। चूंकि पशुओं में बहुत सी प्रजातियां एसी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं इस लिए बढ़ती जनसंख्या के चलते पशुओं के अधिक प्रयोग से पशु भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि दुनिया के कुछ भागों में खाद्य पदार्थ के उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संघ ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि दुनिया के बहुत से इलाक़ों में इंसानों की संख्या वहां आहार के उत्पादन के लिए मौजूद संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक है। इस लिए यदि दुनिया की वर्तमान जनसंख्या का संरक्षण करना है तो खाद्य पदार्थों के संसाधन बढ़ाने होंगे। वरना दूसरी स्थिति में मानव समाज के लिए अनगिनत समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिनमें ग़रीबी, भुखमरी और कुपोषण का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है।
पशुओं के प्रजनन के बारे में जो अनुसंधान किए गए उनसे पता चलता है कि सभी जानवर पर्यावरण संसाधनों के अनुपात में प्रजनन करते हैं। विभिन्न प्रकार के मानव समाजों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि अतीत से ही आहार और इंसानों की संख्या और आहार की उपलब्धि तथा इंसानों के प्रजनन में सीधा संबंध रहा है। जिन समाजों में खाद्य पदार्थ की कमी थी वहां इंसानों का प्रजनन भी कम रहा है। लेकिन अब दुनिया में खेतीबाड़ी में विस्तार हो गया है और प्राकृतिक संसाधनों में भी हस्तक्षेप हुआ है जिसके नतीजे में हर क्षेत्र में इंसानों की जनसंख्या वहां के प्राकृतिक संसाधनों के स्तर से ऊपर पहुंच चुकी है। यह समस्या ग़ैर विकसित देशों में अधिक विकट रूप में सामने आ रही है।
जनसंख्या में वृद्धि और साथ ही साथ विकासशील देशों में ग़रीबी और पर्यावरण के पतन में तेज़ी का मानव जीवन पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तथा टिकाऊ विकास प्राप्त करने की इन देशों की कोशिशें नाकाम रही हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ग़रीब वर्ग का जीवन स्तर लगातार नीचे आता जा रहा है और यह चीज़ भुखमरी तथा जीवन को उत्थान के मार्ग पर ले जाने के संसाधनों के अभाव केरूप में सामने आती है। इन समाजों में मौजूद ग़रीबी पर्यावरण को नुक़सान पहुंचाती है और नुक़सान पहुंचाने की इस प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका अधिक होती है। इस लिए कि महिलाएं अपना तथा अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग करने पर मजबूर होती हैं।
आकंड़ों के अनुसार विकासशील देशों में आकस्मिक मौतों में 40 प्रतिशत मौतों का सबंध संक्रामक रोगों, जन्मजात बीमारियों तथा गर्भ के भीतर ही भ्रण का जीवन समाप्त हो जाने से होता है। जबकि विकसित देशों में इन कारणों से मौतों की दर पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसमें यूं तो अनेक कारकों की भूमिका होती है लेकिन जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि जिसके चलते आहार की कमी होती है और और जल तथा मिट्टी का प्रदूषण बढ़ता है, बीमारियों के स्थानान्तरण और स्वास्थ्य समस्याओं का प्रमुख कारण है।
घनी आबादी वाले बहुत से क्षेत्र, विशेष रूप से वह क्षेत्र जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी स्थिति में नहीं है, संक्रामक रोगों के फैलने का अनुकूल स्थान माने जाते हैं। उदाहरण स्वरूप डेंगी बुख़ार जो मच्छर और पानी के माध्यम से फैलता है घनी आबादी वाले शहरों में बड़ी तेज़ी से अपना असर दिखाता है। प्रतिवर्ष 3 से 9 करोड़ लोगों को यह रोग लगता है जबकि वर्ष 1980 के बाद से इस दर में लगातार ख़तरनाक हद तक वृद्धि हो रही है। यह बीमारी तथा अन्य संक्रामक बीमारियां विश्व भर में ने वाली कुल मौतों के 35 प्रतिशत का मुख्य कारण हैं। दुनिया की 80 प्रतिशत संक्रामक बीमारियां सबसे पहले पानी से पैदा होती हैं जबकि विकासशील देशों में यह दर 90 प्रतिशत तक है। हर साल 2 अरब लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दस्त हो जाता है जबकि इनमें चालीस लाख एसे होते हैं जिनकी मौत हो जाती है अलबत्ता इनमें अधिकतर संख्या बच्चों और नवजात शिशुओं की होती है।
विकासशील देशों में पानी के प्रदूषण की एक और बुनियादी वजह ड्रेनेज के पानी का जलाशयों में पहुंचना है। जैसे कि भारत के 3119 शहारों में से केवल 209 शहर एसे हैं जहां अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है जहां गंदा पानी ज़मीन की सतह पर मौजूद पानी में नहीं मिलता। इनमें आठ ही शहर एसे हें जहां यह व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। चूंकि शहरों में सतह पर पाया जाने वाला पानी पीन और नहाने धोने के लिए प्रयोग होता है इस लिए मलेरिया जैसे रोगों का फैलना स्वाभाविक है। सालाना 50 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं और इनमें 73 लाख लोगों की मौत हो जाती है।
आबादी बढ़ने का एक और बुरा नतीजा हवा का प्रदूषण है जो हर साल करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित करता है। आबादी बढ़ने के कारण रासायनिक पदार्थों का प्रयोग भी बढ़ता है और ईंधन भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आबादी बढ़ने और ईंधान का प्रयोग बढ़ने से हर साल 6 अरब टन कार्ब और 3 अरब 22 करोड़ टन कार्बोनिक गैस वायुमंडल में शामिल हो जाती है। हालिया कुछ दशकों के दौरान आबादी बढ़ने, टेक्नालोजी में आने वाले बदलाव और उन पदार्थों का प्रयोग बढ़ने से जिनसे कार्बन डायआक्साइड गैस पैदा होती है इस गैस के उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति की दर से एक दशमलव दो प्रतिशत बढ़ी है। अध्ययनों से पता चलता है कि आबादी बढ़ना वायुमंडल में दो तिहाई कार्बन डाय आक्साइड बढ़ने का कारण है। चीज़ों का प्रयोग बढ़ने और तकनीकी विकास के कारण एक तिहाई कार्बन डाय आक्साइड गैस पैदा होती है। आबादी बढ़ने से ठोस कूड़ा भी बढ़ रहा है। इस लिए कि कूड़े की मात्रा चीज़ों के प्रयोग की मात्रा पर निर्भर होती है। जंगलों का कटना, मरुस्थलों का दायरा बढ़ना, उपजाऊ ज़मीनों का बंजर हो जाना, पेस्टीसाइड के प्रयोग में वृद्धि, पौधशाला गौसों के कुप्रभाव जैविक विविधता के लिए पैदा होने वाले ख़तरे भी आबादी बढ़ने से पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के उदाहरण हैं।
अलबत्ता इस समय इस बारे में मतभेद है कि आबादी बढ़ने से पर्यावरण को नुक़सान पहुंचता है। कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि पर्यावरण में आने वाला बदलाव आबादी बढ़ने के कारण नहीं है बल्कि चीज़ों के हद से ज़्यादा प्रयोग और टेक्नालोजी के कारण है। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों ही विचार सही माने जा सकते हैं। विकसित देशों में टेक्नालोजी से पर्यावरण को नुक़सान पहुंच रहा है जबकि विकसशील देशों में ग़रीबी और जनसंख्या का बढ़ना पर्यावरण को नुक़सान पहुंचा रहा है। अतः दोनों ही कारक चिंता जनक हैं। जनसंख्या में वृद्धि और टेक्नालोजी दोनों से पर्यावरण को नुक़सान पहुंच रहा है। इस लिए हर क्षेत्र के पर्यावरण की क्षमताओं और संसाधनों को देखकर आर्थिक तथा जनसंख्या संबंधी रणनीति अपनाना ज़रूरी है।