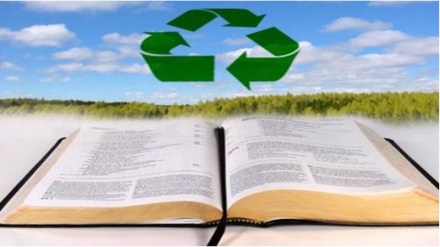हम और पर्यावरण-22
जलवायु परिवर्तन का अर्थ है जलवायु की सामान्य स्थिति में अपेक्षित पैटर्न में बदलाव को कहते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या पूरी दुनिया में लंबे समय तक होता है।
जलवायु परिवर्तन ज़मीन के वायुमंडल में असमान्य बदलाव को दर्शाता है और उसका परिणाम धरती के विभिन्न हिस्सों पर ज़ाहिर होता है। जलवायु परिवर्तन और धरती का बढ़ता तापमान इतना गंभीर मसला है कि 2015 में दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष पेरिस बैठक में उपस्थित हुए ताकि पर्यावरण से जुड़ी इस समस्या का कोई हल निकालें।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल आईपीसीसी ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन है, एक रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के परिणाम की समीक्षा पेश की और पहली बार इस बात के ठोस सुबूत पेश किए कि किस तरह जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तरी ध्रुव में मिट्टी की जमी हुयी परतें और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, महासागरों में कोरल रीफ़ की उत्पत्ति का स्रोत ख़त्म हो रहा है, गर्मी की भीषण लहर चल रही है, बाढ़ लाने वाली वर्षा हो रही है और भारी तूफ़ान आ रहे हैं। 2600 पेज पर आधारित इस रिपोर्ट को तय्यार करने में तीन साल लगे। इस रिपोर्ट को तय्यार करने में दुनिया भर के लगभग 300 वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। इस रिपोर्ट में 230 से ज़्यादा बार ख़तरा शब्द का इस्तेमाल हुआ और इस रिपोर्ट में जिस चीज़ को सबसे बड़ा ख़तरा कहा गया है वह प्राकृतिक आपदताओं व मानव त्रासदियों की संख्या का बढ़ना है। आईपीसीसी के प्रमुख राजेन्द्र पचौरी के शब्दों में, दुनिया में कोई भी जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम से सुरक्षित नहीं बचेगा।
आईपीसीसी सन 2000 से अब तक अमरीका और यूरोप में गर्मी की अभूतपूर्व भीषण लहर सहित बहुत सी त्रासदियों और ऑस्ट्रेलिया में व्यापक स्तर पर आग लगने और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में निवाशकारी बाढ़ के कारण की समीक्षा कर रही थी। इस पैनल के सदस्यों का मानना है कि ध्रुव के ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र के जलस्तर का बढ़ना, जलवायु परिवर्तन के कारण है। इस त्रासदी से सबसे ज़्यासदा ग़रीब, बूढ़े और बच्चे प्रभावित होंगे। दूसरी ओर चूंकि कुछ सरकारों ने ख़ास तौर अविकसित देशों की सरकारों ने इन परिवर्तनों पर अधिक ध्यान नहीं दिया और इससे निपटने के लिए कोई कोशिश नहीं की है इसलिए इन सरकारों को बहुत जल्द विनाशकारी ख़तरों का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण न सिर्फ़ यह कि ग़रीबी बढ़ेगी और खाद्य पदार्थ के स्रोतों में कमी आएगी बल्कि इसकी वजह से बहुत सी जंगें होंगी। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन कर्ताओं और शरणार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में खाद्य पदार्थ के स्रोत में कमी हो रही है और यदि यह प्रक्रिया इसी तरह जारी रही तो गेंहू और मकई के उत्पादन में इतनी कमी आ जाएगी कि उस का प्रभाव महसूस होने लगेगा। इस परिवर्तन का परिणाम अभी भी अफ़्रीक़ा और कैरिबियाई क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। इस रिपोर्ट में इसी प्रकार दुनिया के जलस्रोतों पर भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। दुनिया में समुद्र के जलस्तर के बढ़ने के कारण बहुत बड़ा भूभाग पानी में चला जाएगा और समुद्र के पानी में अम्ल बढ़ जाएगा। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की मछलियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इन प्रजातियों के विलुप्त होने से खाद्य दुनिया भर के लोगों के लिए खाद्य स्रोत में कमी आएगी।
विश्व बैंक ने भी अभी हाल में अपनी रिपोर्ट में सचेत किया कि अगर धरती के बढ़ते तापमान के प्रभाव को सीमित करने के लिए गंभीर क़दम न उठाए गए तो 2030 तक दुनिया में बहुत ज़्यादा ग़रीबी की ज़िन्दगी गुज़ारने वालों की संख्या 10 करोड़ और बढ़ जाएगी। शोध के अनुसार, इसका प्रभाव अफ़्रीक़ा महाद्वीप में ज़्यादा होगा क्योंकि इस महाद्वीप में जलवायु परिवर्तन के कारण इस महाद्वीप में खाद्य पदार्थ की क़ीमत 12 फ़ीसद बढ़ जाएगी जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक होगा क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों की आय का 60 फ़ीसद हिस्सा खाद्य पदार्थ की आपूर्ति में ख़र्च होता है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, “दक्षिण एशिया भी जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र में शामिल है। मिसाल के तौर पर भारत में कृषि उत्पाद में कमी और विभिन्न प्रकार की बिमारियों के तेज़ी से फैलने के कारण भारत में साढ़े चार करोड़ लोग अत्यधिक ग़रीबी के दलदल में फंस जाएंगे। यहां तक कि ये लोग एक दिन में 1 डॉलर और 90 सेंट से कम दैनिक आय पर जीवन गुज़ारने पर मजबूर होंगे।”
विश्व बैंक की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के लोगों के स्वास्थ्य पर पढ़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी सचेत किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा कराए गए शोध के अनुसार, औद्योगिक क्रान्ति से पहले के दौर की तुलना में धरती के तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि दुनिया में 15 करोड़ से ज़्यादा लोग मलेरिया से ग्रस्त होंगे। यह ऐसी हालत में है कि इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 15 साल में उन बीमारियों में 10 फ़ीसद वृद्धि होगी जिन बीमारियों में लूज़ मोशन या दस्त आने की समस्या होती है। विश्व बैंक ने इस बात पर बल देते हुए कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर को कम करने के लिए विश्व स्तर पर तुरंत क़दम उठाकर लाखों लोगों को ग़रीबी से बचाया जा सकता है, दुनिया के अमीर देशों से मांग की कि वे दूसरे देशों की धरती के बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम करने की दिशा में पैसों की मदद करे।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, 146 देशों के मौजूदा रूप में कार्यक्रम से धरती के बढ़ते तापमान को रोकने का लक्ष्य नहीं हो सकता। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ता जाएगा लेकिन पिछले दो दशक की तुलना में वृद्धि कम होगी। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ को विशेषज्ञों ने सचेत किया था कि मौजूदा प्रक्रिया के 2100 तक जारी रहने की स्थिति में धरती का तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और समुद्र का जलस्तर 26 से 82 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने इन देशों के कार्यक्रमों को धरती के तापमान के दो डिग्री से कम बढ़ने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में व्यवहारिक कहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2100 तक ग्रीस हाउस गैसों और कार्बन डाईऑक्साइड गैस का उत्सर्जन शून्य तक पहुंच जाए, वरना मौजूदा प्रक्रिया के उस समय तक जारी रहने की स्थिति में धरती के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का घनत्व दो से तीन गुना बढ़ जाएगा।
जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कमी, स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पूंजिनिवेश, गाड़ियों को हाइब्रिड बनाना, पत्थर के कोयले, गैस और तेल से चलने वाले बिजली घरों में उत्पादित कार्बन गैसों के उत्जसर्न पर रोक और ऊर्जा के उपभोग में किफ़ायत वे उपाय हैं जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को रोकने के लिए पेश किए गए हैं। वन कटाई को रोकना, पब्लिक यातायात के लिए कम प्रदूषण फैलाने वाले साधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना, छोटे-छोटे शहरों को बसाना इस संदर्भ में पेश किए गए अन्य उपाय हैं।
हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशों की ओर से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने से संबंधित पेश किए गए कार्यक्रम के संबंध में संतोष जताया है लेकिन यह बिन्दु भी महत्वपूर्ण है कि इन कार्यक्रमों के लागू होने के बावजूद धरती का तापमान अट्ठारहवीं शताब्दी के औद्योगिक दौर से पहले की तुलना में 2.7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु परिवर्तन मामलों में कार्यकारी सचिव क्रिस्टीना फ़ीगर्स का कहना है कि देशों के ये कार्यक्रम 2100 तक धरती के तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वृद्धि न होने दें लेकिन यह किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है।
इस बात में शक नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के ख़िलाफ़ अभियान सफल नहीं हो सकता। इस सच्चाई की ओर ईरानी राष्ट्रपति डाक्टर हसन रूहानी ने न्यूयार्म में जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में अपने भाषण में संकेत किया था। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा था, “अगर हम इस बात को मान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, तो हमें इस बात को भी मानना होगा कि इससे निपटने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है।” ईरानी राष्ट्रपति ने पर्यावरण समस्या को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए हानिकारक बताते हुए स्पष्ट किया, “अभी से सूखा, पानी की कमी और पर्यावरण समस्या ख़ास तौर पर शहरों में वायू प्रदूषण से निपटने में देशों के पास मौजूद ज्ञान व अनुभव की प्राप्ति कुछ देशों के लिए कठिन हो गयी है। सिर्फ़ चेतावनी और अनुशंसाओं से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को दूर नहीं किया जा सकता बल्कि हमें आर्थिक मेकनिज़्म पर आधारित एक व्यापक सहमति की ज़रूरत है जिसमें सभी देशों के विकास से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान दिया गया हो।”
संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दुनिया के विभिन्न देशों के कार्यक्रम को धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि मानता है जो पेरिस में 2015 में 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलने वाली बैठक का विषय था।