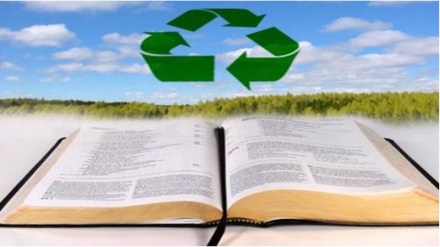हम और पर्यावरण- 24
ओज़ोन की परत बहुत ही संवेदनशील प्राकृतिक गैस का रक्षा कवच है जिसे O3(ओ थ्री) कहा जाता है जो लगभग 25 से 40 किलोमीटर ज़मीन के उपर पाई जाती है।
यह जीवन दायक गैस फिल्टर का काम करती है ओज़ोन ऐसी गैस है जिसमें आक्सीजन के तीन अणु पाये जाते हैं। यह सूरज की पराबैंगनी किरणों को, जो ज़मीन के लिए हानिकारक होती हैं, ज़मीन पर नहीं आने देती है। ओज़ोन गैस की परत लगभग उसी समय से है जब से ज़मीन पर प्राणी है यानी जब से ज़मीन पर ऑक्सीजन पैदा करने वाली चीज़ें व प्राणी अस्तित्व में आये हैं उसी समय से वायुमंडल में O3 गैस अस्तित्व में आई और उस समय यह बहुत ऊपर थी और उसके ऊपर होने के कारण सूरज की पराबैंगनी किरणें बहुत कम मात्रा में ज़मीन की सतह पर पहुंच पाती थीं और ज़मीन के सूखे भागों पर अधिक जीवन की संभावना उत्पन्न हो गयी। ओज़ोन गैस की इस परत में बहुत सी किरणें समाकर ख़त्म हो जाती हैं और वे इस परत को पार नहीं कर पाती हैं परंतु जहां ओज़ोन गैस की परत की मोटाई कम हो गयी है और वहां से सूरज की पराबैंगनी व हानिकारक किरणें पार करके ज़मीन पर आ सकती हैं उसे परिभाषा में ओज़ोन में छेद हो जाना कहा जाता है। अगर ओज़ोन की परत नष्ट हो जाये तो ज़मीन पर जीवन भी समाप्त हो जायेगा और मानव पीढ़ी, जीव- जन्तु और वनस्पतियां कुछ ही समय में नष्ट हो जायेंगी। क्योंकि सूरज की वे किरणें भी ज़मीन पर आ जायेंगी जो जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इनमें से कुछ किरणों में दूसरी चीज़ों के अंदर समा जाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनमें से कुछ किरणें त्वचा की उपरी सतह को पार करके शरीर के अंगों के अंदर पहुंच कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और उन्हें त्वचा के कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारण समझा जाता है। इंसान के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर हो जाना और आंखों में मोतियांबिन्द का हो जाना इन्हीं किरणों का एक दुष्परिणाम है। इसी प्रकार पराबैंगनी किरणें सूक्ष्म जीवों के भी मृत्यु का कारण बनती हैं। ओज़ोन की परत में छेद होने के परिणाम में पराबैंगनी किरणें अनियंत्रित रूप में ज़मीन पर पहुंचती हैं जिससे ज़मीन के तापमान में वृद्धि होती है और उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में बर्फों के पिघलने और सागर के जल स्तरों में वृद्धि का कारण बनता है और परिणाम स्वरूप ज़मीन के सूखे क्षेत्रों के पानी के नीचे चले जाने का कारण बनता है। इसके अलावा ओज़ोन की परत में छेद हो जाना पेड़ पौधों के धीमी गति से बढ़ने का कारण बनता है और जीवित वस्तुओं का जैनेटिक या आनुवंशिक बनावट बिगड़ जाती है और चावल के खेतों में नाइट्रोजन पैदा करने वाले बैक्टिरिया खत्म हो जाते हैं जो फसल की पैदावार में कमी का कारण बनता है। इस मामले में किये गये शोधों से इस बात की पुष्टि हुई है कि ओज़ोन में 25 प्रतिशत ख़राबी आने से समुद्र की उपरी सतह पर रहने वाले 10 प्रतिशत जीव- जन्तु खत्म हो जायेंगे और नदी आदि में रहने वाले 25 प्रतिशत जीव- जन्तु समाप्त हो जायेंगे। ओज़ोन में छेद हो जाने का खेदजनक का रहस्योदघाटन दक्षिणी ध्रुव के अंटारक्टिका क्षेत्र में 1979 से 70 के दशक में हुआ। यह रहस्योदघाटन BAS नामक गुट ने किया। वर्ष 1985 में ओज़ोन की परत में छेद हो जाने से इस सीमा तक चिंता व्याप्त हो गयी कि वैज्ञानिक यह समझ रहे थे कि पर्यावरण की जांच करने वाले उपकरण ही खराब हो गये हैं। वैज्ञानिकों ने पुराने उपकरणों के स्थान पर नये उपकरणों को लगाया परंतु इन उपकरणों से पहले वाले परिणामों की पुष्टि हुई। कुछ महीनों के बाद ओज़ोन में छेद हो जाने को देखा जा सकता था। इसके बाद 1980 में ज़मीन के उत्तरी भाग में ओज़ोन की परत में 15 से 20 प्रतिशत की कमी आई। इसके बाद वर्ष 2006 में ओज़ोन में सबसे अधिक खराबी आई परंतु इन सबसे अधिक ओज़ोन में चिंताजनक खराबी नासा की वह रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि ओज़ोन का दो तिहाई भाग 2065 तक न केवल दक्षिणी ध्रुव बल्कि सारी दुनिया पर तबाह हो जायेगा और इस प्रकार आशंका इस बात की है कि ओज़ोन के छेद के बड़ा होने से ज़मीन पर रहने वाले प्राणियों के जीवन को ख़तरा हो जायेगा। यह समस्त बातें एक ओर परंतु अब यह देखना है कि कौन सी चीज़ें ओज़ोन में छेद होने का कारण बनती हैं?
वैज्ञानिकों के अनुसार ओज़ोन की परत के पतला होने में जो चीज़ें सबसे अधिक प्रभावी हैं वे इस प्रकार हैं” ज़मीन पर परमाणु परीक्षण, ज्वालामुखी पहाड़ियों का फटना और क्लोरोफ्लोरो कार्बन्ज़ जिन्हें सीएफसी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1974 में वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि कुछ कार्बन्ज़ जो घरों, दुकानों, कूलरों आदि और इसी प्रकार प्लास्टिक की चीज़ों में प्रयोग होते हैं, प्रतिक्रिया की योग्यता रखते हैं और जब सीएफसी गैसें वायुमंडल में ऊपर जाती हैं तो सूरज की रौशनी से मिलने पर क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। क्लोरीन एक क्रमबद्ध क्रिया –प्रतिक्रिया द्वारा ओज़ोन को शीघ्र ही नष्ट करने की योग्यता रखती है। इस प्रकार से कि क्लोरीन का एक अणु ज़मीन तक पहुंचने से पहले ओज़ोन के एक लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा सीएफसी गैसें जब बड़े पैमाने पर एकत्रित हो जाती हैं तो ज़मीन के वायुमंडल में रुक जाती हैं और रियेक्शन के बाद ओज़ोन को नष्ट करने लगती हैं। क्लोरीन का प्रयोग विभिन्न प्रकार की साज- सज्जा की स्प्रे बनाने में भी होता है। पर्यावरण के लिए हानिकारक होने के कारण क्लोरीन के प्रयोग को विभिन्न देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है या उसका प्रयोग कम हो गया है।
स्वीडन वह पहला देश है जिसने 23 जनवरी वर्ष 1978 को स्प्रे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इससे ओज़ोन को नुकसान पहुंचता है। ओज़ोन को खराब होने से बचाने के लिए हर साल विभिन्न देशों के वैज्ञानिक विभिन्न कांफ्रेन्सों और सेमीनारों में भाग लेकर अपने- अपने शोधों के परिणामों से एक दूसरे को अवगत कराते हैं। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की कांफ्रेन्सों की ओर संकेत किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने ओज़ोन की रक्षा के लिए वर्ष 1985 में वियना कन्वेन्शन बुलाया था जिसके नतीजे में वर्ष 1987 में विश्व के देशों की सहायता से मॉन्ट्रियाल प्रोटोकोल पारित किया गया। इस प्रोटोकोल के अनुसार विकसित देशों ने वादा किया था कि वे ओज़ोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों जैसे सीएफसी, कार्बन टटरा क्लोराइड और हेलान्स गैसों का उत्पादन नहीं करेंगे और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकासशील देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता भी करेंगे। इसी प्रकार मोन्ट्राल प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करने के बाद जो देश इस कन्वेशन में शामिल हुए हैं उन्होंने अपने तैयार किये गये स्प्रे पर ओज़ोन को नुकसान न पहुंचाने वाला लेबिल लगाने का वादा किया था।
विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया के देश वियना कन्वेशन और मॉन्ट्रियाल प्रोटोकोल का पालन करें और एक समय सारणी के अंतर्गत ओज़ोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों की पैदावार बंद कर दें तो ओज़ोन अपनी प्राकृतिक स्थिति में पलट आयेगा और उसमें जो छेद हुए हैं वे भी भर जायेंगे। अलबत्ता इस कार्य में कम से कम 50 वर्ष का समय लगेगा।
संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव बान की मून ने वर्ष 2015 में ओज़ोन की रक्षा में अंतरराष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में अपने संदेश में कहा था कि यही अंतिम दिनों तक मानवता अपनी ही बनाई गयी त्रासदी के मुहाने पर थी। उन्होंने कहा था कि ओज़ोन को तबाह करने वाली चीज़ें जैसी क्लोरो फ्लोरो कार्बन्ज़ ओज़ोन में जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखती हैं, छेद का कारण बनी हैं लेकिन हमने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए नीतियां अपना ली हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि तीस साल पहले दुनिया ने वियना कन्वेशन पर हस्ताक्षर किया था जिसका लक्ष्य ओज़ोन की रक्षा करना था और अब मोन्ट्रियाल प्रोटोकाल को अपना कर दुनिया क्लोरो फ्लोरो कार्बन सहित ओज़ोन को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे पदार्थों की पैदावार में कमी लाने पर एकजुट हो चुकी है। बान की मून ने अपने संदेश में कहा था कि हम एक दूसरे की सहकारिता व सहयोग से ओज़ोन की परत को जारी शताब्दी के दूसरे पचास वर्षों में बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप चर्म कैंसर के 20 लाख मामलों को रोका जा सकेगा और प्रतिवर्ष लाखों लोगों को मोतिया बिन्द से भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव बान की मून ने अपने संदेश में ओज़ोन की रक्षा के लिए भविष्य में अपने कार्यक्रम की ओर संकेत करते हुए कहा कि हम वर्ष 2030 तक के विकास कार्यक्रम की स्वीकृति और उसके पालन की प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने कहा कि जारी वर्ष के अंतिम दिनों में पेरिस सम्मेलन में सरकारों के क्रिया- कलापों के दृष्टिगत मोन्ट्रियल प्रोटोकोल की सफलताएं हमारे लिए प्रेरणादायक होनी चाहिये। बान की मून के कथनानुसार यह सफलता उस समय हमारी क्षमता की सूचक है जब राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय चुनौती का मुकाबला करने के लिए एकजुट रूप में काम कर रहे हैं किन्तु मोन्ट्रियल प्रोटोकोल का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। हाइड्रा फ्लोरो कार्बन का प्रयोग ओज़ोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ के स्थान पर किया जा रहा है इसके बावजूद कि इस प्रकार की चीज़ों से ओज़ोन की परत को नुकसान नहीं पहुंचता है परंतु आज भी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में मौजूद हैं और यदि हम अभी से प्रभावी कार्य नहीं करते हैं तो हमारी ज़मीन का तापमान बढ़ता जायेगा। मोन्ट्रियल प्रोटोकोल के अंतर्गत राजनीतिक संकल्प से हाइड्रा फ्लोरो कार्बन को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की गयी है और यह मौसम के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है और अगर एसी ही इच्छा शक्ति दोबारा प्राप्त हो जाये तो पर्यावरण की रक्षा के लिए किये जाने वाले प्रयास भी सफल हो जायेंगे। ओज़ोन की रक्षा के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर आइये सब मिलकर प्रण करते हैं कि जिस तरह से हमने ओज़ोन की रक्षा की है उसी तरह अपने पर्यावरण व जमीन की भी रक्षा करेंगे किन्तु इसकी रक्षा के लिए केवल नारों से काम नहीं चलेगा बल्कि देशों के मध्य सहकारिता भी ज़रूरी है और यह चीज़ उस समय व्यवहारिक होगी जब वर्चस्ववादी देश विश्व के दूसरे लोगों व देशों के हितों के बारे में सोचेंगे।