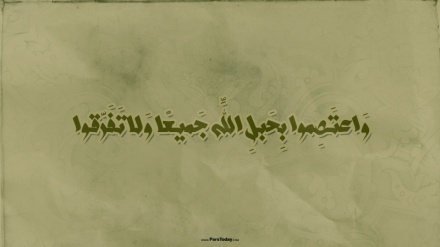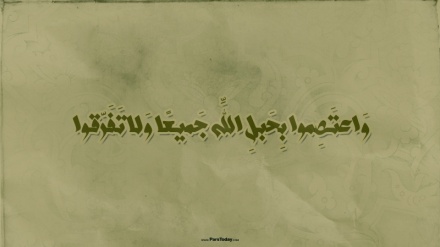इस्लामी जगत- 19
इस्लामी जगत की एकता पर राष्ट्रवाद के अनुभव ने सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव यह डाला कि उसे तीन भागों, अरबी, ईरानी और तुर्की में बांट दिया।
पश्चिम में चर्च और शासकों के बीच संबंधों से उत्पन्न होने वाले शासनों के साथ ही, इस्लामी साम्राज्य के स्तर पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप इस साम्राज्य का पतन हो गया और इस्लामी जगत में राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरूआत हुई।
उस समय तक इस्लामी जगत में इस्लाम स्वीकार करने वालों के लिए कोई सीमितता नहीं थी, कोई भी मुसलमान अपने जन्म स्थान से उठकर इस्लामी जगत के किसी भी देश में जाकर बस सकता था, लेकिन मुग़लों और तैमूर के हमलों के कारण और बग़दाद में अब्बासी ख़िलाफ़त के पतन के बाद, इस्लामी साम्राज्य तीन भागों में बंट गया, अरबी, ईरानी और तुर्की।
दूसरा अनुभव उन्नीसवीं शताब्दी के शुरूआती दशकों से संबंधित है। इस काल में राष्ट्रवाद फ़्रांसीसी क्रांति और रूमांटिक साहित्य से प्रभावित था, जिसने उस्मानी शासन के अंदर विरोधी विचारधारओं के लिए भूमि प्रशस्त की। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि न्यू उस्मानी सुधारवादियों के तुर्क राष्ट्रवाद, कैथोलिक प्रचारकों एवं चर्चों के प्रचार, आंतरिक उथल पथल और विदेशी हमलों ने उस्लामी शासन के पतन के लिए भूमि प्रशस्त की।
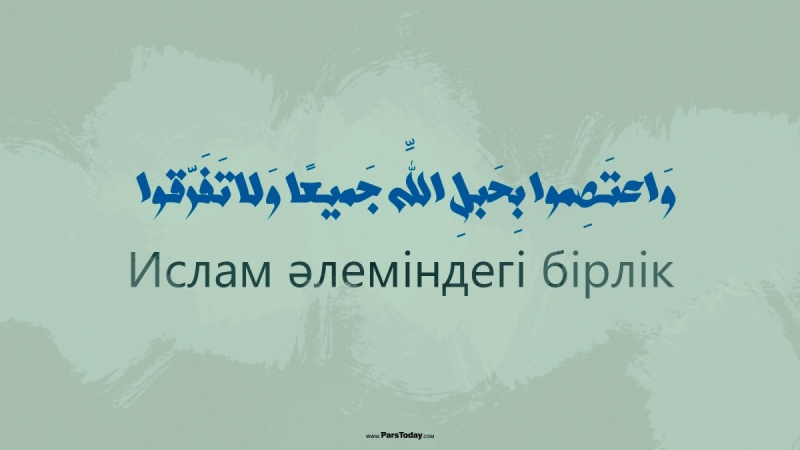
उस्मानी शासन के पतन के नतीजे में बुल्गारिया में विद्रोह, उस्मानी शासन और रूस के बीच युद्ध, उस्मानी शासन से बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो का अलग होना और पान अरबिज़्म उस्मानी शासन के पतन का परिणाम थे। इस काल में पान तुर्किज़्म और पान अरबिज़्म के स्वरूप में राष्ट्रवाद ने वैचारिक एवं सांस्कृतिक रूप से राजनीतिक एवं सामाजिक रूप ले लिया और उसने केवल विशेष अवसरों पर वह भी अस्थायी रूप से पश्चिमी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ प्रतिक्रिया दिखाई।
एक दूसरा अनुभव इस शताब्दी के अंत से संबंधित है। इस काल में यद्यपि सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय धार्मिक भावनाएं भड़का कर इस्लामी जगत में एकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे, युवा तुर्क आंदोलकारियों ने न्यू उस्मानी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए 1889 में एकता एवं विकास समिति का गठन किया और सुल्तान के पतन के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने मश्वरत अख़बार निकालकर तुर्कों की भावनाओं को भड़काया और उनसे एकजुटता का आहवान किया। इन आंदोलनकारियों ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के साथ ख़ुफ़िया संपर्क स्थापित कर, उस्मानी शासन के पतन के लिए ताक़त के इस्तेमाल की योजना तैयार की और सुल्तान अब्दुल हमीद के ख़िलाफ़ विद्रोह शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सुल्तान ने पान इस्लामिज़्म का सहारा लिया, हालांकि यह प्रयास विफल रहा और 1908 में सुल्तान का पतन हो गया।
तुर्क राष्ट्रवाद के मुक़ाबले में अरबों को अपनी सांस्कृतिक पहचान की चिंता हुई, इसी कारण अरब विद्वानों ने अरब पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए पान अरबिज़्म का नारा दिया। इसी के साथ नजीब आज़ूरी जैसे लोगों के प्रयासों से तूरानिज़्म के मुक़ाबले में अरब राष्ट्रवाद की बुनियाद रखी। बीसवीं शताब्दी में मीशल अफ़लक़ के विचारों और अरब समुदाय की एकजुटता के नारे के साथ यह आंदलोन आगे बढ़ा।
बीसवीं शताब्दी में भी इस्लामी जगत में राष्ट्रवाद में तेज़ी आई। इस शताब्दी के पहले अर्ध में इस्लामी जगत में विभिन्न देशों ने जन्म लिया। पहले विश्व युद्ध के बाद अरब अलग अलग राष्ट्रीय ईकाईयों में बंट गए और इराक़, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों के गठन के साथ आपसी प्रतिस्पर्दा और दुश्मनी की शुरूआत हुई। दूसरी ओर फ़ार्स खाड़ी में कुवैत और क़तर जैसे छोटे देशों का गठन हुआ। पाकिस्तान, भारत से और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। पूर्वी अफ़्रीक़ा के तटीय देश, जहां मुसलमान बहुसंख्या में थे, छोटे छोटे देशों में बंट गए, इस प्रकार इस्लामी समुदाय विभाजित और टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी प्रकार, देशों के भीतर सामुदायिक राष्ट्रवाद का शक्तिकरण हुआ और एक ही देश में तुर्क, कुर्द, अरब और बलोच एक दूसरे से उलझ पड़े, इस प्रकार सामुदायिक पहचान धार्मिक पहचान पर हावी हो गई और इस्लामी जगत की एकता बिखर गई।
राष्ट्रवाद की तरह ही तानाशाही शासकों ने इस्लामी जगत की एकता को नुक़सान पहुंचाया। जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में इशारा किया था कि सैय्यद जमालुद्दीन असदाबादी और अब्दुर्रहमान कवाकिबी जैसे इस्लामी जगत के सुधारवादियों के अनुसार, अलोकतांत्रिक एवं तानाशाही सरकारें, इस्लामी जगत में एकता के मार्ग में एक बड़ी रुकावट रही हैं।
सैय्यद जमालुद्दीन का मानना था कि ग़ैर तानाशाही सरकारें, जातीय और राष्ट्रीय भावनाओं को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर, समाज में एकता उत्पन्न करती हैं। जमालुद्दीन की तरह कवाकिबी का भी मानना था कि मुसलमानों में राजनीतिक चेतना की कमी और उसके परिणाम स्वरूप तानाशाही सरकारों का गठन, इस्लामी देशों के पिछड़ेपन का कारण है। वे आंतरिक अत्याचार को इस्लामी समाजों की मूल समस्या बताते थे, इस प्रकार इस्लामी जगत के पिछड़ेपन और साम्प्रदायिकता को शासकों के अत्याचारों में खोजते थे।
इस्लामी देशों के इतिहास में कई ऐसे अवसर हैं, जिससे पता चलता है कि तानाशाह शासकों ने इस्लामी जगत में साम्प्रदायिकता को हवा दी है। यहां इस बिंदु पर ध्यान देना उचित होगा कि तानाशाही की परिभाषा राजनीतिक विज्ञान के अन्य विषयों की भांति धेड़ी जटिल है, इसीलिए इसकी ऐसी परिभाषा कि जिस पर सब सहमत हों, कठिन है। उदाहरण स्वरूप स्पष्ट नहीं है कि किस हद तक दबाव, हिंसा और केन्द्रीकरण तानाशाही के दायरे में आएगा। इसलिए कि हर देश में एक सरकार है और दबाव एवं हिंसा प्रत्येक शासन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि देश को चलाने के लिए शक्ति और हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन किस प्रकार तानाशाही शासनों को ग़ैर तानाशाही शासनों से अलग कर सकते हैं?
डेमोक्रेटिक शासन और तानाशाही शासन के बीच अंतर करने के लिए दो चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली यह कि तानाशाही शासन हिंसा और बल के आधार पर वजूद में आता है, दूसरे शब्दों में सत्ता पर निंयत्रण के लिए चुनावों का सहारा नहीं लिया जाता है। दूसरे यह कि इस व्यवस्था में सत्ता सामान्य रूप से एक व्यक्ति या एक पार्टी के निंयत्रण में होती है, इसीलिए फ़ैसले भी इसी आधार पर होते हैं। इसी कारण इस प्रकार की व्यवस्था में नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को महत्व नहीं दिया जाता है। फ़ैसले भी जनता के हितों के बजाए डिक्टेटर के हितों को मद्देनज़र में रखकर किए जाते हैं। दुनिया भर के तानाशाही शासन भी विचारधार, सैन्य या असैन्य व्यवस्था और सत्ता हड़पने के लिए प्रयोग की गई शक्ति के आधार पर विभिन्न हैं, लेकिन समस्त तानाशाही शासनों के बीच उल्लेख की गई दो बातें सामान्य होती हैं।
इतिहास गवाह है कि इस्लामी जगत में इस प्रकार के शासनों ने इस्लामी देशों के बीच एकता के मार्ग में रुकावटें खड़ी की हैं। इसलिए कि तानाशाहों के फ़ैसलों और जनता की मांगों के बीच कोई समानता नहीं होती और उन्हें अन्य इस्लामी सरकारों के साथ संबंध मज़बूत बनाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे यह कि इन सरकारों को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए दोनों की महत्वकांक्षाएं भिन्न होती हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्था में अगर समस्त इस्लामी देशों की जनता सहयोग और एकता में रूची रखती होगी तो भी यर सरकारें इस विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगी।
तीसरे यह कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों के ग़ैर इस्लामी और तानाशाही अंदाज़ के कारण, इस्लामी देशों की जनता उनके साथ सहयोग करने पर विश्वास नहीं रखती है। इस्लामी देशों के शासकों पर जनता का विश्वास न होने के कारण इस्लामी एकता नष्ट हो जाती है। यहां हम इसके कुछ उदाहरण पेश कर रहे हैं।
जब उस्मानी ख़िलाफ़त के केन्द्र में जातीय और राष्ट्रीय भेदभाव ने जड़ पकड़ ली थी और एक ओर विभिन्न समुदायों और गुटों के बीच तनाव था और दूसरी ओर उस्मानी साम्राज्य इस्लामी जगत के दूसरे ध्रुव अर्थात सफ़वी ईरान से टकरा रहा था, सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने पान इस्लामिज़्म का नारा लगाया और इस्लामी देशों के बीच रिश्ते मज़बूत बनाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने इन देशों के बीच रेलवे लाईन बिछाने और पवित्र मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों के स्वागत जैसे क़दम उठाए। हालांकि इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट उस्मानी शासन के भीतर उनकी तानाशाही नीतियां थीं। दूसरे शब्दों में मुसलमानों के साथ सुल्तान के तानाशाही रवैये और ग़ैर इस्लामी व्यवहार के कारण वह जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके, इसीलिए यह क़दम उनके राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए समझे गए, जिसके कारण उनका पान इस्लामिज़्म आइडिया विफल हो गया।
इसी प्रकार 1970 के दशक में जब फ़िलिस्तीन के मुद्दे को लेकर इस्लामी जगत में एकजुटता बन रही थी और अधिकांश इस्लामी देश इस्राईल से टकराने के लिए एकजुट थे, ईरान की तानाशाही सरकार ने यूरोप और पश्चिम पर तेल के प्रतिबंध के आंदोलन में शामिल न होकर 1973 में इस एकता को भंग कर दिया। इस टकराव में इस्लामी और अरबी देश इस्राईल के मुक़ाबले में एकजुट थे, लेकिन ईरान के शाह ने इस्राईल और अमरीका के साथ साज़िश करके इस एकता की प्रगति में रुकावट डाल दी। इसलिए कि ईरानी शाह एक अत्याचारी तानाशाह था और ईरानी जनता के विचार उसके लिए महत्व नहीं रखते थे, इसी कारण उसने इस्लामी देशों का साथ नहीं दिया और इस्लामी जगत में एकजुटता का सुनहरा अवसर बर्बाद कर दिया।
इसी प्रकार, ईरान में शाह के शासन के पतन और इस्लामी क्रांति की सफलता के समय, इस्लामी जगत में एकता के लिए भूमि प्रशस्त हुई और ईरान सोवियत संघ, अमरीका और इस्राईल के मुक़ाबले में इस्लामी जगत में एकता में रूची रखता था, सद्दाम ने ईरान पर हमला करके ईरान के विरुद्ध अरबों की राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का दिया और इस्लामी जगत में एकता स्थापित नहीं होने दी। अब सद्दाम के शासन के पतन और इराक़ में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद इस्लामी जगत में एकता के लिए भूमि प्रशस्त हुई है, लेकिन कुछ देशों की तानाशाही सरकारें हस्तक्षेप करके मुसलमानों की एकता में विघ्न डाल रही हैं।