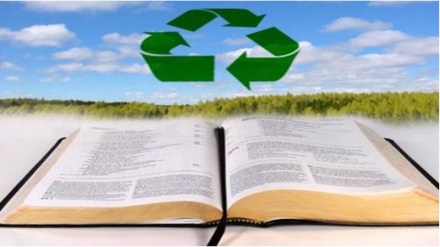हम और पर्यावरण- 38
टिकाऊ विकास शब्द सबसे पहले 1970 के दशक में प्रयोग किया गया जिसका तात्पर्य हर उस गतिविधि में स्थिरता लाना है जिसमें स्रोतों और विकल्प की ज़रूरत होती है।
वस्तुतः टिकाऊ विकास वह विकास है जो आगामी पीढ़ियों की क्षमताओं को नुक़सान पहुंचाए बिना किसी भी समाज की मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करे। इस परिभाषा में दूसरी पीढ़ियों द्वारा प्राकृतिक स्रोतों से लाभान्वित होने जितनी ही मात्रा से लाभ उठाने के हर पीढ़ी के अधिकार को औपचारिकता दी गई है और प्राकृतिक पूंजि से आवश्यकता भर ही लाभ उठाने को वैध बताया गया है। इस आधार पर टिकाऊ विकास, एक ऐसा तत्व है जो समाप्त होने वाले संसाधनों में स्थिरता का कारण बनता है। ये सीमित संसाधन धरती पर आने वाली आगामी पीढ़ियों के जीवन के लिए आवश्यक हैं। टिकाऊ विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव समाजों के लिए वांछित भविष्य निश्चित कर सकती है। ऐसा भविष्य जो, जीवन के हालात और संसाधनों का प्रयोग, जीवन की आवश्यक व्यवस्था की अखंडता, सुंदरता व स्थिरता को क्षति पहुंचाए बिना, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।
इस आधार पर टिकाऊ विकास, मनुष्य व प्रकृति और इसी तरह इंसानों के आपसी संबंध को समझने में एक अहम परिवर्तन है। यह ऐसा विषय है जो पिछली दो शताब्दियों में, पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के विषयों को अलग-अलग करने के मनुष्य के दृष्टिकोण से विरोधाभास रखता है। पिछली दो सदियों में पर्यावरण को एक बाहरी और केवल मनुष्य के प्रयोग के तत्व के रूप में देखा जाता था। इस दृष्टिकोण में, जो पूंजिवाद और औद्योगिक क्रांति के विकास से संबंधित था, यह सोचा जाता था कि मनुष्य हर स्थिति में प्रकृति को अपने अधीन रख सकता है। यहां तक कि नवीन विज्ञान के एक जनक बेकन का भी मानना था कि संसार, इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान संसार के लिए नहीं। निश्चित रूप से उद्योग व विज्ञान के विकास ने मनुष्य के जीवन के मानकों को बेहतर बनाने और उसके ज्ञान में वृद्धि में मूल भूमिका निभाई है। आवास, आहार, परिवहन, शिक्षा-प्रशिक्षण, अनुसंधान और चिकित्सा सेवा जैसी सारी चीज़ें विज्ञान व औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई हैं लेकिन इसके साथ अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि औद्योगिक विकास के मानक, जिनमें पर्यावरण की ज़रूरतों को दृष्टिगत नहीं रखा गया है, अस्थिर मानक हैं। इस आधार पर आज की दुनिया में और विकास से संबंधित कार्यक्रमों में औद्योगिक विकास और पर्यावरण की स्थिरता दो मूल तत्व हैं।
टिकाऊ विकास, ढांचागत, सामाजिक और आर्थिक विकास के नश्वर मानकों के लिए समाधान पेश करता है ताकि प्राकृतिक स्रोतों की तबाही, जैविक तंत्रों की बर्बादी, प्रदूषण, मौसम में परिवर्तन, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि, अन्याय, जीवन स्तर घटने जैसी समस्याओं को रोका जा सके। इस आधार पर टिकावऊपन और स्थिरता एक ऐसी स्थिति है जिसमें समय बीतने के साथ संसाधन और उनकी गुणवत्ता कम नहीं होती बल्कि यह अनंत भविष्य में भी संसाधनों के बाक़ी रहने के लिए पर्यावरण की क्षमताओं से संबंधित होती है।
इस विषय के महत्व के दृष्टिगत और पर्यावरण के बारे में वैश्विक चिंताओं के निवारण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पर्यावरण के लिए मौजूद ख़तरों पर चर्चा के लिए पहली बैठक आयोजित की। इस सम्मेलन में धरती की परिस्थितियों की रक्षा के लिए सार्वजनिक प्रयास, सीमा पर प्रदूषण के बारे में देशों के दायित्व और विकास के अधिकार और राष्ट्रीय स्रोतों के बारे में देशों की स्वाधीनता और प्रभुसत्ता जैसे मामलों के समाधान के लिए कुछ सिद्धांत पेश किए गए। पर्यावरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा बड़ा सम्मेलन, जो धरती शिखर सम्मेलन के नाम से भी मशहूर है, वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो शहर में आयोजित हुआ।
इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में “सहस्त्राब्दी घोषणापत्र” संकलित व पारित हुआ। इस सम्मेलन में संसार के 189 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जो बातें स्वीकार की थीं उनमें से एक पर्यावरण की स्थिरता की गारंटी थी। यह सहस्त्राब्दी के विकास के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बात के लिए कटिबद्ध हुए कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने सभी प्रयास करेंगे और अपने अपने देश की नीतियों व कार्यक्रमों में टिकाऊ विकास के सिद्धांतों को शामिल करेंगे और प्राकृतिक स्रोतों की तबाही को रोकेंगे। इसी प्रकार यह भी तै पाया कि पीने का स्वच्छ पानी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों की संख्या कम से कम 50 प्रतिशत तक कम करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना भी सहस्त्राब्दी घोषणापत्र के लक्ष्यों में शामिल था।
हालांकि वर्ष 2000 में बहुत से देश, टिकाऊ विकास के लिए प्रतिबद्ध हुए लेकिन इस दस्तावेज़ को संकलित हुए 16 साल का समय बीत जाने के बावजूद साक्ष्यों से यही पता चलता है कि यह लक्ष्य, अर्थात प्राकृतिक स्रोतों और पर्यावरण की तबाही की प्रक्रिया को रोकना, व्यवहारिक नहीं हो पाया है। उदाहरण स्वरूप यद्यपि पीने के स्वच्छ पानी तक लोगों की पहुंच बढ़ी है लेकिन विकासशील देशों की आधी आबादी, स्वास्थ्य संबंधित आरंभिक संसाधनों से अब भी वंचित है। हालांकि शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन से ग्रामीण क्षेत्रों की ज़मीन पर पड़ने वाला दबाव कुछ कम हुआ है लेकिन इससे झुग्गी झोंपड़ियों, शहरों के आस-पास और असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस समय लगभग एक अरब लोग शहरों के किनारे जीवन बिता रहे हैं क्योंकि शहरी क्षेत्रों की आबादी बढ़ने की रफ़्तार आवास और रोज़गार मिलने की प्रक्रिया से तेज़ है। रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न पशु और वनस्पतियां अभूतपूर्व ढंग से विलुप्त होती जा रही हैं। मौसम बदलता जा रहा है और समुद्रों के पानी में वृद्धि, सूखे और बाढ़ जैसे ख़तरों की आशंका मानव जीवन को संकट में डालती जा रही है।
इसके अलावा पर्यावरण की एक बहुत बड़ी समस्या अर्थात मौसम के परिवर्तन ने पिछले बरसों में अपने कुप्रभाव दिखाने शुरू कर दिए हैं। वर्षा की मात्रा में कमी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है और पानी की भारी कमी होती जा रही है। पानी की कमी इस सीमा तक है कि संबंधित संस्थाओं ने इसे संसार का तीसरा बड़ा ख़तरा बताया है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले चार साल में पानी की कमी, आहार और ऊर्जा की आपूर्ति के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा, देशों और सरकारों को गंभीर संकट में डाल देगी और अनेक देशों को मौसम में परिवर्तन और खाने के स्रोतों में सीमिता के कारण विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के प्रसार से जूझना पड़ेगा। पर्यावरण के विशेषज्ञों ने भी कहा है कि संसार के अधिक वर्षा वाले आधे से अधिक क्षेत्र समाप्त हो चुके हैं और मौसम में आने वाले परिवर्तन ने पूरी दुनिया में मौसम के मानकों को बदल दिया है और इससे पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है।
अलबत्ता यह दुखद स्थिति अधिकतर उन दरिद्र देशों में दिखाई पड़ती है जहां के लोग अपने प्रतिदिन का ख़र्चा चलाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण स्वरूप विकासशील देशों में पर्यवारण संबंधी अधिकतर समस्याओं की जड़ दरिद्रता के कारण है क्योंकि ग़रीबी पर्यावरण की तबाही का कारण बनती है और पर्यावरण की तबाही दरिद्रता में वृद्धि करती है। इसी तरह पर्यावरण संबंधी मामलों के महत्व से आम लोगों की अनभिज्ञता, प्राकृतिक स्रोतों के अधिक इस्तेमाल और प्रदूषण का कारण बनती है। विकासशील देशों के सामने एक और समस्या, औद्योगिक देशों पर उनकी निर्भरता है जबकि विकसित व औद्योगिक देशों की ऊर्जा या कच्चे माल के बड़े भाग की आपूर्ति विकासशील देश करते हैं लेकिन पर्यवारण की सुरक्षा के संबंध में इन देशों की बिल्कुल भी मदद नहीं की जाती।