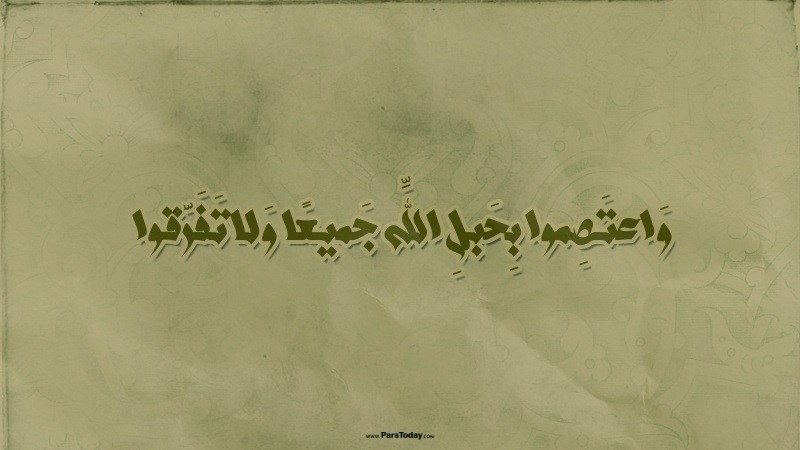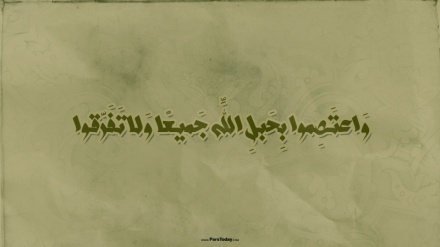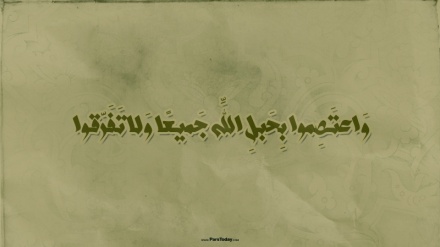इस्लामी जगत-28
हमने विभिन्न कालों में इस्लामी जगत में एकता पैदा करने की दिशा में इस्लामी कांफ़्रेंस संगठन या इस्लामी सहयोग संगठन के गठन और उसके लक्ष्यों के मुद्दे पर चर्चा की थी और इसकी गतिविधियों के चार ऐतिहासिक चरणों के बारे में बताया था।
पहले चरण में यह संगठन फ़िलिस्तीन उद्देश्य के लिए समर्पित था और इस उद्दश्य की प्रगति के लिए इस संगठन ने इस्लामी देशों के बीच एकता पैदा करने की कोशिश थी। इस चरण की विशेषता यह थी कि सदस्य देशों के बीच रुझहान में काफ़ी वृद्धि हुई। तीसरा चरण, इस संस्था का तीसरा चरण वर्ष 1997 में तेहरान कांफ़्रेंस से आरंभ होता है और वर्ष 2011 और 2012 में कुछ अरब देशों में मुसलमानों की क्रांतियां इस काल में शामिल हैं। इस काल में इस्लामी देशों के मध्य ध्यान योग्य एकजुटता में वृद्धि हुई। चौथा चरण, कुछ अत्याचारी शासनों में इस्लामी जागरूकता नामक क्रांतियों की ओर पलटता है जिसमें इस्लामी देशों में मतभेद और विवाद बढ़ा गया और सदस्य देशों के आपस में टकराव बढ़ गये। इस्तांबोल में इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक के घोषणापत्र से इन मतभेदों के चरम पर पहुंचने का पता चलता है।

इस्लामी सहयोग संगठन की गतिविधियों के दूसरे चरण में मुस्लिम देशों के संबंधों में गुप्त वास्तविकताएं सामने आईं जिसके कारण इस संगठन की पहचान के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गयीं। यह मतभेद गंभीर थे जिसने इस संगठन को अपने लक्ष्यों और उमंगों से काफ़ी दूर कर दिया और एक प्रकार से सदस्य देशों के बीच रूढ़ीवाद फैल गया। इराक़ द्वारा ईरान पर हमला, काबे में ईरानी तीर्थयात्रियों को गोलियों की बौछार करके शहीद करना और ओआईसी द्वार सऊदी अरब की इस अमानवीय कार्यवाही का समर्थन, कुवैत पर इराक़ की सैन्य चढ़ाई, बैतुल मुक़द्दस की स्वतंत्रता की उमंगों और फ़िलिस्तीनी जनता के संघर्ष के व्यापक समर्थन से हटना और मिस्र द्वारा ओआईसी से निकलने के बाद संगठन में वापसी जैसी घटनाओं ने इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच मतभेद पैदा कर दिए या दूसरे शब्दों में सदस्य देशों के बीच मतभेद उजागर हो गया है।
यह ऐसी हालत में है कि वर्ष 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में विशेषकर कुवैत पर इराक़ के हमले के समय, इस्लामी देशों के बीच रूढ़ीवाद का घेरा और भी बढ़ गया और तेहरान के इस्लामी सहयोग संगठन के अध्यक्ष बनने के बाद सदस्य देशों के बीच संबंधों की बहाली का नया चरण आरंभ हुआ। यह ऐसी हालत में था कि सोवियत संघ और पूर्वी ब्लाक के विघटन के बाद दुनिया में अकेले खिलाड़ी के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका दुनिया में एक ऐसे विकल्प की तलाश में था जिससे कोई मतभेद न हो और जो पूर्वी ब्लाक का स्थान ले सके और वह इस्लामी जगत के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता था।
हैंटिंग्टन जैसे विचारकों ने सभ्यताओं से टकराव का मुद्दा पेश करके इस टकराव की वैचारिक भूमिका प्रशस्त की। हैंटिंग्टन के दृष्टिकोणों के आधार पर शीत युद्ध की समाप्ति से दुनिया नये चरण में पहुंच गयी है जिसकी मुख्य विशेषता दो श्रुवीय दुनिया की विचारधाराओं के बीच टकराव नहीं है बल्कि सभ्यताओं का टकराव है जिसमें मुख्य टकराव दो सभ्यताओं इस्लामी और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच टकराव था।

इस्लामी गणतंत्र ईरान यद्यपि हमेशा से इस दृष्टिकोण का विरोधी रहा है किन्तु विश्व स्तर पर और मुसलमानों के बीच अस्तित्व में आने वाले वातावरण से उसने मुस्लिम देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करने के लिए इससे भरपूर लाभ उठाया। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने इस संगठन की अध्यक्षता के काल में तेहरान बैठक में पहली बार सभ्यताओं के टकराव से मुक़ाबला करने के लिए सभ्यताओं के बीच वार्ता का दृष्टिकोण पेश किया और विश्व स्तर पर ईरान के इस प्रयास को इतना अधिक सराहा गया कि वर्ष 2001 को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से सभ्यताओं के बीच वार्ता का वर्ष घोषित किया गया है। ईरान के तत्वकालीन राष्ट्रपति ने इस्लामी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आठवीं बैठक में भाषण देते हुए इस्लामी जगत की वास्तविकताओं और इस्लामी देशों के बीच वार्ता और विश्वास बहाली पैदा करने की आवश्यकता के दृष्टिगत, इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए समिति के गठन का सुझाव पेश किया जिसका इस्लामी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भरपूर स्वागत किया।
इस कमेटी ने अपनी बैठकों के दौरान इस्लामी देशों के सदस्यों के बीच राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए कुछ सिद्धांत पेश किए। सदस्य देशों के बीच अविश्वास के माहौल के दृष्टिगत, कमेटी ने सदस्य देशों के बीच एक प्रकार की राजनैतिक व वैचारिक एकता पैदा करने का प्रयास किया। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने इसी प्रकार ओआईसी की अध्यक्षता के दौरान इस्लामी जगत में मौजूद संकटों के समाधान में गंभीर प्रयास किए और एक तरफ़ सदस्य देशों के बीच सहयोग और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करके इस्लामी जगत की समस्याओं को कम करने और इस संगठन के बीच आंतरिक एकता मज़बूत करने का बहुत प्रयास किया।
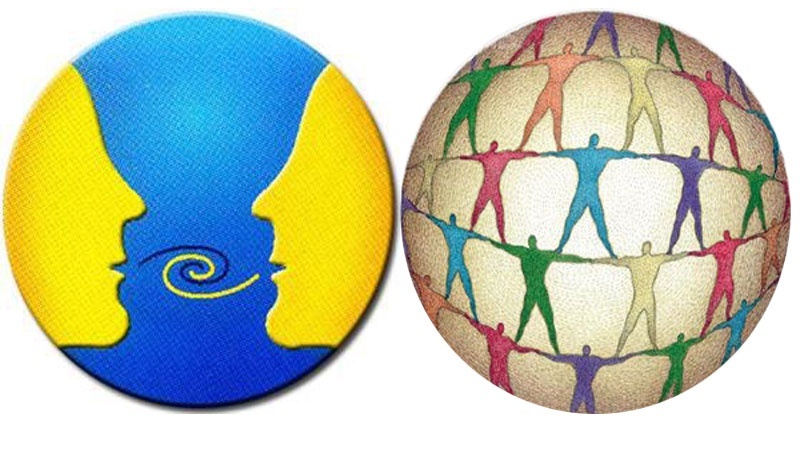
उदाहरण स्वरूप फ़िलिस्तीन के मुद्दे में इस विषय की संवेदनशीलता के दृष्टिगत, ज़ायोनी शासन की आतंकवादी, दमनकारी और विस्तारवादी कार्यवाहियों की निंदा की गयी। इसी प्रकार इस विषय के दृष्टिगत कि इस्राईल ने इस दौरान अपनी विस्तारवादी नीतियों को फिर से आरंभ किया और इस विषय ने इस्लामी जगत की चिंताओं को एक बार फिर से बढ़ा दिया। तेहरान ने एक सक्रिय कूटनीति का सहारा लेते हुए ज़ायोनी शासन से मुक़ाबले के लिए इस्लामी देशों की क्षमताओं से भरपूर लाभ उठाया। ईरान ने ओआईसी की अपनी अध्यक्षता के दौरान सबसे पहले ज़ायोनी शासन की अमानवीय कार्यवाहियों को दुनिया के सामने पेश किया और फिर इस शासन पर भीषण दबाव डालकर यह दिखा दिया कि फ़िलिस्तीन के मुद्दे के प्रति इस्लामी जगत कितना संवेदनशील है। इस प्रकार अध्यक्षता के इस काल में ईरान ने इस्लामी जगत में लेबनान, इराक़, अफ़ग़ानिस्तान, कोसोवो और चेचन्या के संकट के हल के लिए बहुत कोशिश की और इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य देशों और इस्लामी जगत में एकता के लिए उचित पृष्ठिभूमि मुहैया की।
तेहरान बैठक, इस्लामी जगत विशेषकर इस्लामी सहयोग संगठन के लिए राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की बैठक थी। राजनैतिक उपलब्धियों के अतिरिक्त विभिन्न देशों की संस्कृतियों और सभ्यताओं के टकराव को रोकने के लिए वार्ता का क्रम आरंभ हुआ और ईसीओ, संयुक्त राष्ट्र संघ और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो गया और इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया गया। अंतर्रसंसदीय संघ भी उन विषयों में था जिस पर तेहरान बैठक में बल दिया गया। आर्थिक दृष्टि से भी इस बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गये। एक प्रस्ताव मुस्लिम देशों के संयुक्त बाज़ार और दूसरा 21वीं शताब्दी में प्रविष्ट होने के लिए इस्लामी देशों को तैयार करना था। सांस्कृतिक दृष्टि से मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बैठकों का आयोजन, क़मरी महीने की तारीख़ों को समान करना, एक साथ इस्लामी ईदें मनाना और संयुक्त इस्लामी समन्वय समिति के गठन जैसी कार्यवाहियों की ओर संकेत किया जा सकता है।
तेहरान बैठक के बाद भी इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच अच्छे सहयोग की प्रक्रिया जारी रही। इसी मध्य 11 सितंबर 2001 में अमरीका के जुड़वां टावर पर हमला हो गया, इस हमले के बाद से इस्लामी जगत के विरुद्ध अकारण दुश्मनी फैलने लगी किन्तु इससे इस्लामी देशों के बीच एक प्रकार की एकता और एकजुटता भी पैदा हुयी। उदाहरण स्वरूप पश्चिम द्वारा इराक़ पर हमले की धमकी के बढ़ने के बाद इस्लामी सहयोग संगठन ने 5 मार्च 2003 को और लगभग इस हमले से एक महीना पहले ही एक आपातकालीन बैठक आयोजित की और इस बैठक में सदस्य देशों ने इराक़ पर हर प्रकार के संभावित हमले की ओर से सेचत किया और इराक़ की राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में बल दिया गया कि किसी भी मुस्लिम देश को इराक़ पर हमले में भागीदार नहीं होना चाहिए।

वर्ष 1997 से 2011 और 2012 के बीच के काल में बहुत से मुस्लिम देशों में जनक्रांतियां आरंभ हुईं और तब तक इन देशों में एकजुटता पायी जाती थी। इस काल में इस्लामी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कुल मिलाकर छह बैठकें की जिनमें से दो बैठकें आपातकालीन थीं। वर्ष 2000 में आयोजित होने वाली नवीं बैठक में इस्राईल के अतिक्रमण के मुक़ाबले में लेबनानी राष्ट्र की सफलता पर बधाई पेश की गयी। बाद वाली बैठक सऊदी अरब, मलेशिया और सिंगापूर में आयोजित हुई जिनमें सीरिया, लेबनान और फ़िलिस्तीन की निहत्थी व पीड़ित जनता के संबंध में अमरीका और इस्राईल की कार्यवाहियों से जुड़े विषयों पर संयुक्त बयान जारी किए गये। 2008 में आयोजित होने वाली ग्यारहवीं बैठक में लेबनान और फ़िलिस्तीनी जनता के विरुद्ध इस्राईल की अपराधिक कार्यवाहियों की निंदा और सीरिया के विरुद्ध अमरीका के एकपक्षीय प्रतिबंधों की निंदा की गयी और सीरिया को दंडित करने के क़ानून का खंडन किया गया और सीरियाई जनता से सहृदयता व्यक्त की गयी।

15 मार्च 2011 में इस्लामी सहयोग संगठन की 12वीं बैठक मिस्र के शरमुश्शैख़ में आयोजित होने वाली थी किन्तु क्षेत्र में इस्लामी जागरूकता और जनक्रांतियों के आरभ होने से मिस्र में अशांति फैल गयी जिसके कारण यह बैठक न हो सकी। यह घटनाएं भी मुस्लिम देशों के बीच फिर से तनाव पैदा होने और सदस्य देशों के बीच रूढ़ीवाद में वृद्धि का कारण बनीं।