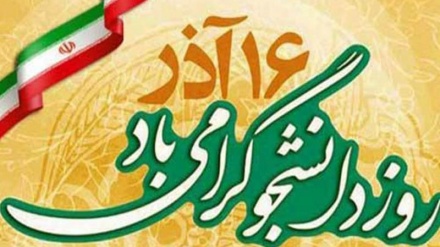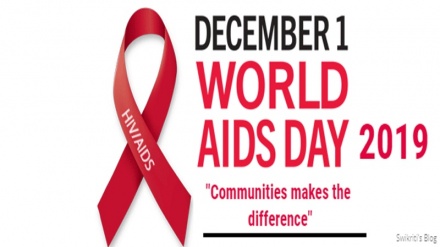इस्लामी क्रांति दूसरा क़दम- 10
ईरान की इस्लामी क्रान्ति फ़रवरी 1979 में आयी और अब इसे 4 दशक से ज़्यादा का समय हो रहा है।
इस दौरान ईरानी जनता ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। अब वह क्रान्ति के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति और देश के विकास के मार्ग पर चल रही है। इस्लामी क्रान्ति के दूसरे चरण का घोषणापत्र जिसे आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामेनई ने इस महाघटना के चालीस साल पूरे होने पर जारी किया, इस्लामी क्रान्ति की आकांक्षाओं के आधार पर ईरान के भविष्य का ख़ाका पेश करता है। लेकिन इन वर्षों की घटनाओं को जाने और मौजूदा स्थिति को समझे बिना स्पष्ट भविष्य की ओर क़दम उठाना न सिर्फ़ यह कि कठिन है बल्कि मुमकिन है क़दम मार्ग से भटक जाए। यही वजह है कि इस्लामी क्रान्ति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामेनई इस घोषणापत्र में इस बात का उल्लेख करते हुए कि जो कुछ क्रान्ति की पहली पीढ़ी ने देखा और अनुभव किया आज की क्रान्तिकारी नस्ल ने न तो देखा और न ही अनुभव किया, बल देते हैः "भविष्य में ठोस क़दम उठाने के लिए विगत की पहचान और अनुभव से पाठ लेना ज़रूरी है। अगर इस नियम की अनदेखी की गयी तो झूठ सत्य की जगह ले लेगा और भविष्य अज्ञात ख़तरों के निशाने पर आ जाएगा।"
यह बिन्दु इस दृष्टि से अहम है कि इस्लामी क्रान्ति की सफलता के आरंभ से ही दुश्मनों ने इस क्रान्ति की छवि ख़राब करने के लिए दुष्प्रचार शुरु किया और इस समय वे इस कोशिश में हैं कि इंटरनेट, सोशल साइटों, रेडियो और टीवी चैनलों के ज़रिए इस्लामी क्रान्ति के ख़िलाफ़ संशय पैदा करें, इसकी उपयोगिता को छिपाएं, कमियों को बड़ा दिखाएं और जनता को इस्लामी क्रान्ति के प्रदर्शन की ओर से निराश करें। यही वजह है कि इस्लामी क्रान्ति के वरिष्ठ नेता क्रान्ति के दूसरे चरण के घोषणा पत्र में बल देते हैं कि क्रान्ति के दुश्मन अतीत और वर्तमान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे और उसके बारे में झूठे दावे कर रहे हैं। वे इस मार्ग में पैसों और दूसरे हथकंडों की मदद ले रहे हैं। विचार, आस्था और जागरुकता के लुटेरे बहुत हैं। सत्य को दुश्मन और उनके किराए के पिछले से नहीं सुना जा सकता।
क्रान्ति के दूसरे चरण के घोषणापत्र में आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामेनई ने, जिन हालात में इस्लामी क्रान्ति सफल हुयी है, और ईरान तथा दुनिया पर उसका क्या असर पड़ा, इस बात को सही तरीक़े से चित्रित करने की कोशिश की है। यह जनांदोलन उस समय शुरु हुआ जब देश पर रक्त पिपासू, तानाशाही और दूसरों का पिट्ठ शासन राज कर रहा था। देश में आज़ादी का कोई वजूद नहीं था और जो लोग शाही शासन की आलोचना का साहस या आज़ादी की कोशिश करते थे, उनका अंजाम जेल, यातना और मौत के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे दमनकारी शासन को पश्चिम ख़ास तौर पर अमरीका का भरपूर समर्थन हासिल था। पश्चिम की सरकारें विरोधियों का दमन करने में शाही शासन की मदद करती और रज़ा शाह और उसके साथियों के आर्थिक व राजनैतिक भ्रष्टाचार में साथ देती थीं। शाही शासन की ओर से थोपे गए घुटन भरे माहौल पर पश्चिमी सरकारें कभी भी आपत्ति नहीं करती थीं जबकि यही पश्चिमी सरकारें ख़ुद को मानवाधिकार व राष्ट्रों की आज़ादी का समर्थक बताती हैं। रज़ा शाह ने इतनी ज़्यादा मात्रा में पश्चिम से हथियार ख़रीदे थे कि उसे सत्ता से हटाने की संभावना मात्र सपना भर थी।

क्रान्ति के दूसरे चरण के घोषणापत्र में आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामेनई लिखते हैः इस्लामी क्रान्ति और इससे वजूद में आयी व्यवस्था ने शून्य से काम शुरु किया। सारे हालात हमारे ख़िलाफ़ थे। चाहे वह भ्रष्ट व उद्दंडी शासन रहा हो जो विदेश पर निर्भर, भ्रष्ट, तानाशाही व सैन्य विद्रोह से वजूद मे आने के अलावा, ईरान में पहला शाही शासन था जो अपनी तलवार की ताक़त के ज़रिए नहीं बल्कि विदेशियों की मदद से वजूद में आया था, चाहे अमरीकी और कुछ दूसरी पश्चिमी सरकारें रहीं हों, चाहे देश के अस्तव्यस्त हालात रहे हों, चाहे विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लज्जाजनक पिछड़ापन रहा हो, चाहे राजनीति, अध्यात्म और दूसरी विशेषताएं रही हों, इन सब दृष्टि से हालात हमारे ख़िलाफ़ थे, लेकिन यही रुकावटें दमनकारी शाही शासन और उसके पश्चिमी समर्थकों के ख़िलाफ़ संघर्ष शुरु व जारी रहने का कारण बनीं।
हर क्रान्ति को सफलता के बाद एक प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। उस दौर की क्रान्तियां प्रायः पूर्व सोवियत संघ में चलने वाली साम्यवादी प्रशासनिक व्यवस्था का पालन करती थीं जो अनेक कमियों की वजह से न सिर्फ़ उन देशों बल्कि ख़ुद पूर्व सोवियत संघ में भी असफल था और अंततः साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो गया। दूसरे देशों में प्रशासनिक मॉडल पश्चिम में प्रचलित पूंजिवादी व्यवस्था पर आधारित है जो बहुत सी कमियों की वजह से इन देशों में त्रुटीपूर्ण तरीक़े से लागू हुआ जिसके नतीजे में उनकी पूंजिवादी सरकारों पर निर्भरता बढ़ गयी। इस बीच ईरान की क्रान्ति का, जो इस्लामी क्रान्ति की प्रतीक है, किसी भी मौजूद प्रशासनिक मॉडल पर भरोसा नहीं था बल्कि वह क्रान्ति के संस्थापक इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्ला अलैह के दिशा निर्देश में इस्लामी व्यवस्था की स्थापना की कोशिश में थी जो अभूतपूर्व घटना थी।

इस्लामी क्रान्ति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामेनई क्रान्ति के दूसरे चरण के घोषणापत्र में इस बात की इस तरह व्याख्या करते हैः "हमारे पास कोई अनुभव नहीं था। स्पष्ट सी बात है कि मार्क्सवादी और उन्हीं की तरह के आंदोलन उस क्रान्ति के लिए आदर्श नहीं हो सकते थे जो ईश्वर पर आस्था और इस्लामी शिक्षाओं के आधार पर वजूद में आया था। इस्लामी क्रान्तिकारियों ने बिना किसी अनुभव के काम शुरु किया और गणतंत्र व इस्लाम का संयोग तथा इसके गठन व प्रगति के लिए साधन ईश्वर की कृपा और इमाम ख़ुमैनी के विचारों से मुहैया हुए और यह क्रान्ति की पहली चमक थी।" इस तरह इस्लामी मूल्यों और जनता की राय पर आधारित एक व्यवस्था अर्थात धार्मिक प्रजातंत्र इस्लामी गणतंत्र के रूप में वजूद में आया।
इस्लामी क्रान्ति जिस समय सफल हुयी उस समय दुनिया में दो ध्रुवीय व्यवस्था क़ायम थी। इस तरह कि अमरीका और पूर्व सोवियत संघ नामी दो शक्तियां और उनके घटक एक दूसरे के मुक़ाबले में लामबंदी किए हुए थे। अमरीका उदारवादी पूंजिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था जबकि सोवियत संघ साम्यवादी मत का समर्थन करता था। इस बीच ईरान की क्रान्ति ने धर्म व अध्यात्म के आधार पर नई प्रशासनिक व्यवस्था का विचार पेश किया और इस तरह तीसरे प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था प्रकट हुयी। भौतिकवादी व्यवस्थाओं का खोखलापन 1991 में साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित सोवियत संघ के विघटन के रूप में सामने आया। इस विघटन से दो साल पहले ही इस्लामी क्रान्ति के संस्थापाक स्वर्गीय इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दूरदृष्टि व आध्यात्मिक शक्ति से इस विघटन को भांप लिया था और इसका कारण उन्होंने पूर्व सोवियत संघ के नेता मीख़ाईल गोर्बाच्योफ़ को ख़त में लिखा था। इमाम ख़ुमैनी ने गोर्बाच्योफ़ को ख़त में लिखा थाः "श्रीमान! गोर्बाच्योफ़। यह बात सबके लिए स्पष्ट हो चुकी है कि अब साम्यवाद को सिर्फ़ दुनिया के राजनैतिक इतिहास के म्यूज़ियम में ढूंढा जाएगा, क्योंकि साम्यवाद इंसान की वास्वतिक ज़रूरतों में से किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। इसका कारण इस मत का भौतिकवादी होना है और भौतिकवाद के ज़रिए मानवता को उस संकट से नहीं निकाला जा सकता जिसमें वह अध्यात्म के बारे में आस्था न रखने की वजह से घिरी हुयी है। आध्यात्मिक संकट पूरब और पश्चिम दोनों समाजों की संयुक्त पीड़ा है।"
आध्यात्म पर आस्था न रखने से उत्पन्न संकट ऐसा संकट है जिसका पश्चिम की उदारवादी पूंजिवादी व्यवस्था को सामना है कि जिसके पतन के चिन्ह स्पष्ट हो चुके हैं। इस्लामी क्रान्ति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामेनई पूर्व सोवियत संघ के पतन के बाद के हालात के बारे में क्रान्ति के दूसरे चरण के घोषणापत्र में कहते हैः "ईरानी राष्ट्र की क्रान्ति ने तत्कालीन दो ध्रुवीय व्यवस्था को तीन ध्रुवीय व्यवस्था में बदल दिया और फिर सोवियत संघ और उसके पिट्ठुओं के पतन के साथ ही शक्ति के नए ध्रुव के सामने आए। इस्लाम और साम्राज्य के बीच तुलना होने लगी जो समकालीन जगत की अहम घटना है और इस ओर दुनिया वालों का ध्यान केन्द्रित हुआ।"
इस्लामी क्रान्ति की सफलता और ईरान में रेफ़्रेन्डम में 98 फ़ीसद जनता के मत से इस्लामी व्यवस्था के क़ायम होने से दुनिया की शक्तियां नाराज़ हुयीं और वे इस नई व्यवस्था को गिराने में लग गयीं। ख़ास तौर पर इसलिए कि इस्लामी गणतंत्र अपने संविधान के आधार पर दुनिया के पीड़ितों का समर्थन करता और इस्लामी जगत के बीच एकता को अपना कर्तव्य समझता है। इस्लामी क्रान्ति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामेनई दुनिया के पीड़ितों पर इस्लामी क्रान्ति के असर और साम्राज्यवादी शक्तियों की प्रतिक्रिया के बारे में कहते हैः "एक ओर पीड़ित राष्ट्र, दुनिया में आज़ादी चाहने वाले आंदोलनों और स्वाधीनता की इच्छुक सरकारों की निगाहें क्रान्ति की ओर उठीं तो दूसरी ओर दुनिया की साम्राज्यवादी शक्तियों ने द्वेषपूर्ण नज़रों से क्रान्ति को देखा। इस तरह दुनिया का मार्ग बदल गया और क्रान्ति के भूंचाल से साम्राज्यवादियों की नींद उड़ गयी और फिर पूरी ताक़त से दुश्मनी शुरु हुयी।"

साम्राज्यवादी मोर्चे ने पृथकतावादी विद्रोह, राजनैतिक संकट उत्पन्न करने से लेकर सैन्य विद्रोह कराने की कोशिश की, पाबंदी लगायी और जंग छिड़वा दी। इस बीच इराक़ के तानाशाह सद्दाम की कमान में और उसके पश्चिमी व अरब समर्थकों की छत्रछाया में ईरान पर थोपी गयी आठ वर्षीय जंग से ईरान को भारी नुक़सान पहुंचा लेकिन इस जंग में उसे हार हुयी। इसके बाद अमरीका और उसके योरोपीय घटक ने ईरानी राष्ट्र के ख़िलाफ़ आर्थिक पाबंदियां कड़ी कर दीं ताकि उसे क्रान्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक दें लेकिन ईश्वर की कृपा, क्रान्ति की आकांक्षाओं व इस्लामी क्रान्ति के संस्थापक और इस्लामी क्रान्ति के नेता से जनता की निष्ठा से दुश्मन की राजनैतिक, सैन्य, आर्थिक और प्रचारिक साज़िशें नाकाम हो गयीं। आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामेनई क्रान्ति के दूसरे चरण के घोषणापत्र के इस भाग का इन शब्दों में निष्कर्ष पेश करते हैः अब जबकि क्रान्ति का वार्षिक जश्न चालीस बार मना चुके और चालीस स्वतंत्रता प्रभात का उदय हो चुका है, दुश्मनी के दो ध्रुवों में से एक साम्यवाद ख़त्म हो चुका है और दूसरी ओर उदारवाद भी अपनी मुश्किलों की वजह से अंतिम सांसे ले रहा है, इस्लामी क्रान्ति अपने नारों की रक्षा और उसके प्रति वफ़ादारी के साथ निरंतर आगे बढ़ती जा रही है।