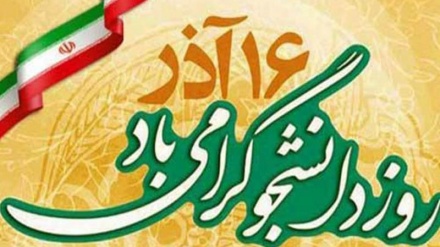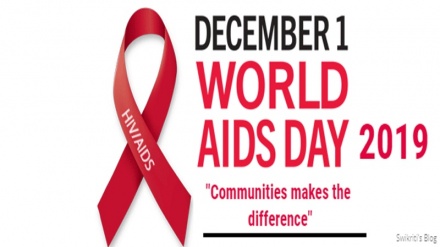ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी प्रतिबंध- 1
लगभग 40 साल से जबसे ईरान में 1979 में इस्लामी गणतंत्र ईरान की स्थापना हुयी, अमरीका विभिन्न बहानों से ईरान पर पाबंदी लगाता रहा है।
ये पाबंदियां पहले तेहरान में अमरीकी दूतावास को नियंत्रण में लेने के बहाने लगायी गयीं हालांकि अमरीकी दूतावास पर नियंत्रण ईरान में अमरीकी हस्तक्षेप और पहलवी शासन को 25 साल से अमरीकी समर्थन का जवाब था लेकिन तेहरान में अमरीकी दूतावास पर नियंत्रण के मामले के ख़त्म होने और अलजज़ाएर घोषणापत्र के जारी होने के बाद अमरीकियो ने इस नीति को आतंकवाद का समर्थन, मानवाधिकार का उल्लंघन और सामूहिक विनाश के हथियार की प्राप्ति के बहाने उस समय जारी रखा जब ईरान की भूमि पर इराक़ के पूर्व बासी शासन ने अतिक्रमण कर रखा था और ईरान की अपनी रक्षा के लिए हथियारों तक पहुंच को रोक दिया गया था।
इसके बाद ईरान का शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम अमरीका की अगुवाई में पश्चिम की व्यापक व कठोर पाबंदियों का बहाना बना। अमरीकियो ने इस एलान के साथ कि वे ईरानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, पाबंदियों के इतिहास में ईरान के ख़िलाफ़ सबसे कठोर पाबंदियां लगायीं और उसे स्मार्ट पाबंदियों का नाम दिया। उन्होंने बड़ी शक्तियों को अपने साथ मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस्लामी गणतंत्र ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों के कई प्रस्ताव पारित कराए और अपनी प्राथमिक व दूसरे दर्जे की पाबंदियों को वैश्विक पाबंदियों में बदल दिया। इसके बावजूद इस्लामी गणतंत्र ईरान ने परमाणु ऊर्जा से लाभ उठाने के अपने मूल अधिकार की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियां जारी रखीं यहां तक कि बड़ी शक्तियां इस अधिकार को मानते हुए ईरान के साथ वार्ता की मेज़ पर आयीं।
ईरान और गुट पांच धन के बीच जिसमें अमरीका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ़्रांस और जर्मनी शामिल हैं, लगभग 2 साल की सघन बातचीत के बाद जेसीपीओए नामक परमाणु समझौता वजूद में आया जिसमें सामने वाले पक्ष ईरान की ओर से कुछ बातों की पाबंदी के बदले में उसके ख़िलाफ़ परमाणु पाबंदियों को निरस्त या स्थगित करने पर बाध्य हुए, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के सत्ताकाल में अमरीकी नए बहाने से ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों को अपनी विदेश नीति के हथकंडे के तौर पर बाक़ी रखना चाहते हैं।
जैसा कि कार्यक्रम के शुरु में हमने यह बताया कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका की ओर से पहली आर्थिक पाबंदी 1980 में तेहरान में अमरीकी दूतावास पर ईरानी छात्रों द्वारा नियंत्रण की घटना की प्रतिक्रिया लगायी गयी। इस पाबंदी के तहत ईरान के पूर्व शासक मोहम्मद रज़ा पहलवी के शासन काल में करोड़ों डॉलर के सैन्य उपकरणों की बिक्री से संबंधित समझौता निरस्त और इस्लामी गणतंत्र ईरान को सैन्य उपकरणों की बिक्री को ग़ैर क़ानूनी घोषित किया गया। इस घोषणा के बाद, अमरीका में ईरान सरकार की संपत्ति से 12 अरब डॉलर को ज़ब्त कर लिया गया और ईरान-अमरीका के बीच हर प्रकार के व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगा दी गयी। इसी प्रकार अमरीकी सरकारने इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ अपने सभी कूटनैतिक संबंध तोड़ लिए।
तत्तकालीन अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की सरकार ने जो ईरान में इस्लामी क्रान्ति की सफलता और उसके बाद तेहरान में अमरीकी दूतावास पर छात्रों के नियंत्रण की घटना से बहुत क्रोधित थी, इन पाबंदियों से बड़ी उम्मीद लगा रखी थी। इस्लामी क्रान्ति की सफलता से पहले तक ईरान का आर्थिक ढांचा पूरी तरह अमरीका पर निर्भर था। देश की ज़रूरी चीज़ों का बड़ा भाग जिसमें खाद्य पदार्थ, दवा से लेकर औद्योगिक ज़रूरतों की चीज़े, उपभोग की वस्तुओं को आपूर्ती पश्चिम से और ख़ास तौर पर अमरीका से होता था। यही स्थिति ईरान के सशस्त्र बल के संबंध में थी जिस पर क्रान्ति के संवेदनशील में सुरक्षा की आपूर्ति की ज़िम्मेदारी थी। पहलवी शासन काल में सेना की सारी ज़रूरत की चीज़ें अमरीका से आयात होती थीं और अमरीकी यह सोचते कि तेहरान-वॉशिंग्टन के बीच व्यापारिक व सैन्य संबंध के टूटने से अंत में ईरानी राष्ट्र इस्लामी क्रान्ति के मूल्यों से हट जाएगा। इसके बावजूद क्रान्ति के नेतृत्व व ईरानी राष्ट्र ने यह फ़ैसला किया कि जब तक उचित लगेगा अमरीकी बंधकों को तेहरान में रोके रखेंगे यहां तक वॉशिंग्टन ईरान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने की ईरानी जनता की मांग के सामने झुक जाए।
यह मांग अलजज़ाएर नामक घोषणापत्र के जारी होने और अमरीकी सरकार की ओर से ईरान के मामले में हस्तक्षेप न करने के लिखित वादे के साथ व्यवहारिक हुयी और अंततः 444 दिन के बाद अमरीकी बंधक अपने देश लौटे, लेकिन तेहरान में बंधक मामले के ख़त्म होने के बावजूद ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों का क्रम न रुका। अलबत्ता ज़ाहिरी तौर पर अलजज़ाएर घोषणापत्र के जारी होने के बाद अमरीका ने अपने योरोपीय घटकों के साथ यह एलान किया कि उसने उन पाबंदियों को निरस्त कर दिया है जो तेहरान में बंधक घटना के बाद लगायी थीं लेकिन वॉशिंग्टन ने अमरीकी कंपनियों की मांगों के बहाने और ईरान द्वारा ख़रीदे गए सैन्य उपकरणों की सुपुर्दगी पर रोक लगा कर इन पाबंदियों को और व्यापक स्तर पर जारी रखा। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका की नई पाबंदियों की व्यापकता के चिन्ह जनवरी 1984 में स्पष्ट होना शुरु कि उस समय ईरान ने इराक़ की बासी सेना के मुक़ाबले जंग के मोर्चों पर बड़ी सफलताएं हासिल की थीं।
तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रॉनल्ड रीगन ने ईरान के ख़िलाफ़ इराक़ द्वारा थोपी गयी 8 साल की जंग के दौरान, ईरान को सैन्य उपकरण की ब्रिक्री पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की ताकि इस तरह ईरान को इराक़ के ख़िलाफ़ जंग में जीतने से रोक सके। जनवरी 1984 में वॉशिंग्टन ने बैरूत में अमरीकी नौसैनिक ठिकाने में हुए धमाके के बहाने जिसमें 241 लोग मारे गए थे, इस्लामी गणतंत्र ईरान का नाम आतंकवाद के समर्थक देशों की सूचि में शामिल किया। उसके बाद से आतंकवाद का समर्थन करने का इल्ज़ाम ईरान के ख़िलाफ अमरीकी पाबंदियों को व्यापक स्तर पर लगाने का बहाना बन गया। लगभग दो साल बाद इसी बहाने ईरान को अमरीका की ओर से हर प्रकार के सैन्य उपकरणों की बिक्री व निर्यात पर रोक लग गयी और ईरान को ऐसी वस्तुओं के निर्यात की निगरानी होने लगी जो सैन्य और असैन्य दोनों आयाम से इस्तेमाल हो सकती थीं। इसी तरह अमरीकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों जैसे विश्व बैंक में अपने प्रतिनिधि को नोटिस भेजा कि वे इन संगठनों को ईरान को किसी भी तरह का क़र्ज़ देने से रोकें और इसी तरह इन संगठनों को अपनी वित्तीय मदद में उस हद तक कमी कर दी जिस हद तक ये संगठन ईरान को पैसे क़र्ज़ दे सकते थे। इसके साथ ही ईरानी राष्ट्र से अमरीकी सरकार की दुश्मनी बढ़ती गयी। वर्ष 1987 में रीगन सरकार ने झूठे बहानों से ईरान को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया जो मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग़ैर क़ानूनी व्यापार में लिप्त हैं और इस तरह इस्लामी गणतंत्र ईरान को सैन्य उपकरणों की बिक्री व निर्यात के मार्ग में और रुकावटें खड़ी कर दीं। अमरीका ने यह क़दम ऐसी हालत में उठाया था कि ईरान अफ़ग़ानिस्तान से मादक पदार्थ की होने वाली तस्करी के ख़िलाफ़ संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में है और इस मार्ग में उसने बड़ी संख्या मे शहीदों का बलिदान दिया है।
यह स्थिति 1988 में ईरान-इराक़ जंग के अंत तक जारी रही। अलबत्ता ईरान मे पुनर्निर्माण का दौर शुरू होते ही इस्लामी गणतंत्र ईरान और योरोपीय संघ के बीच आर्थिक व राजनैतिक संबंध बेहतर होने लगे लेकिन अमरीका न सिर्फ़ यह कि योरोप के साथ न हुआ बल्कि उसने अपनी पाबंदियां भी बढ़ा दीं। मिसाल के तौर पर हेग के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने अमरीका को यह आदेश दिया कि उसने पहलवी शासन के दौर में सैन्य समझौते के तहत जो क़रीब 30 करोड़ डॉलर पेशगी लिए हैं, उसे लौटाए लेकिन इसके बावजूद वॉशिंग्टन ने 1991 में ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबंदियां लगायीं। क्षेत्र के तेज़ी से बदलते हालात के मद्देनज़र अमरीकियों ने ईरान के ख़िलाफ़ अपनी पाबंदी की नीति और कड़ी कर दी। कुवैत पर इराक़ के अतिक्रमण के बहाने जिसके बाद अमरीका ने इराक़ पर चढ़ाई कर दी, अमरीकियों ने नई पाबंदियां लगायीं। 1992 में "ईरान और इराक़ में सैन्य उपकरणों के विस्तार पर रोक" नामक क़ानून लागू हुआ हालांकि 1991 में अमरीका-इराक़ जंग में जो फ़ार्स खाड़ी की पहली जंग के नाम से मशहूर है, ईरान के हस्तक्षेप न करने से अमरीकियों के लिए जीत का रास्ता तेज़ी से समतल हुआ। अलबत्ता इस्लामी गणतंत्र ने अपनी सैद्धांतिक नीति के तहत संवेदनशील क्षेत्र पर हर प्रकार के अतिक्रमण को बुरा समझते हुए कुवैत के अतिग्रहण के संकट में दाख़िल होने से परहेज़ किया। ईरान की इस सैद्धांतिक नीति का अमरीकियों ने दुश्मनी से जवाब दिया।
बिल क्लिंटन की अध्यक्षता में अमरीका की नई सरकार ने द्विपक्षीय कंट्रोल शीर्षक के तहत एक नीति संकलित की जिसका लक्ष्य ईरान और इराक़ को एक साथ नियंत्रित करना एलान किया गया। तत्कालीन अमरीकी अधिकारियों को इस बात की चिंता थी कि फ़ार्स खाड़ी की पहली जंग के बाद इराक़ के कमज़ोर होने से ईरान कहीं क्षेत्र की शक्ति न बन जाए और पश्चिम एशिया में अमरीकी हित ख़तरे में न पड़ जाएं। इसी वजह से पिछली पाबंदियों के साथ साथ अमरीकी अधिकारियो ने नई पाबंदियां लगायीं ताकि ईरान की विदेशी आय का मुख्य स्रोत अर्थात तेल की बिक्री प्रभावित हो। लेकिन चूंकि ईरान के तेल के निर्यात पर रोक लगाने से तेल मंडी में तूफ़ान आ जाता, अमरीकियों ने ईरान के तेल व गैस उद्योग में पश्चिमी कंपनियों के पूंजिनिवेश को रोकने की चाल चली। जो चीज़ क्लिंटन की सरकार की पाबंदी की नीति को पिछली वाली सरकारों की नीति से अलग ज़ाहिर करती थी वह पाबंदियों के दायरे का अमरीका से निकल कर इस देश की सीमाओं के बाहर बढ़ना था।