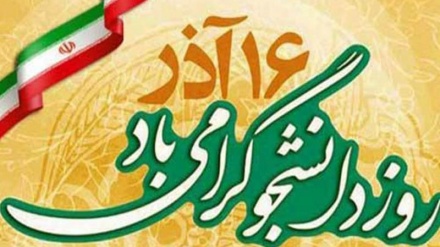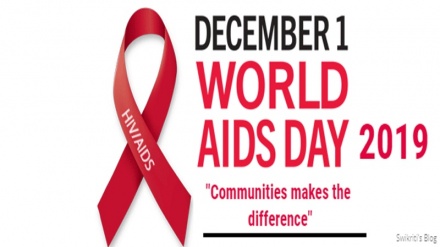ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी प्रतिबंध- 2
आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने आपको इस्लामी गणतंत्र ईरान के संबंध में अमेरिका की प्रतिबंधों की नीति आरंभ होने के अतीत के बारे में बताया था।
उस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि तेहरान में ईरानी छात्रों द्वारा अमेरिकी दूतावास पर नियंत्रण कर लेने के बहाने अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। यह 1980 का वह समय था जब ईरान की इस्लामी क्रांति को सफल हुए एक वर्ष का समय बीत चुका था। यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि अमेरिकी सरकार द्वारा शाह की अत्याचारी सरकार के समर्थन करने और इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ जासूसी के अड्डे में परिवर्तित होने के बाद ईरानी छोती ने अमेरिकी दूतावास पर नियंत्रण किया था। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाया था उसके अनुसार कोई अमेरिकी नागरिक ईरान से व्यापार नहीं कर सकता था, अमेरिका में ईरान की सम्पत्ति को रोक लिया गया और इसी तरह ईरानी राष्ट्र के पैसे से शाह की सरकार ने अमेरिका से जो हथियार खरीदे थे अमेरिका ने उसे भी ईरानी राष्ट्र को नहीं दिया।
अलजज़ाएर घोषणापत्र जारी व पारित होने और अमेरिका द्वारा ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित वचन देने के बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास के कूटनियकों को बंधक बनाये जाने का मामला समाप्त हो गया पर इसके बाद अमेरिका ने ईरान द्वारा आतंकवाद के समर्थन जैसे विषय का बहाना बनाया और उसकी आड़ में तेहरान के विरुद्ध वाशिंग्टन की प्रतिबंधों की नीति को जारी रखा। यह प्रतिबंध उस समय में जारी रहा जब इराक ने ईरान पर युद्ध थोप रखा था और ईरानी सेना को अपनी रक्षा के लिए हथियारों की ज़रूरत थी। अमेरिका ने उस संवेदनशील समय में भी ईरान को हथियार नहीं दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि अमेरिका ईरानी राष्ट्र को घुटने टेक देने पर बाध्य कर देना चाहता था और इसी कारण वह ईरान के हाथों हर प्रकार के हथियारों की बिक्री के मार्ग में बाधा बन गया। अमेरिका ने इराक द्वारा ईरान पर थोपे गये युद्ध के दौरान इराक की बासी सरकार का व्यापक समर्थन किया यहां तक कि जब इराक ने ईरान के खिलाफ युद्ध आरंभ कर रखा था उस समय फार्स की खाड़ी में ईरान के तेल के प्रतिष्ठानों और इसी प्रकार फार्स की खाड़ी में जा रहे ईरान के यात्री विमान पर हमला करने में भी अमेरिका ने संकोच से काम नहीं लिया। ज्ञात रहे कि फार्स की खाड़ी में अमेरिका ने ईरान के जिस यात्री विमान को लक्ष्य बनाया था उसमें 290 यात्री शहीद हो गये थे।
वर्ष 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था। उस समय भी ईरान के संबंध में अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीति परिवर्तित नहीं हुई जबकि ईरान ने सिद्धांतिक नीति अपनाई और वह इस विवाद में शामिल नहीं हुआ। इसके बावजूद फार्स की खाड़ी युद्ध में इराक की पराजय के बाद और बिल क्लिंटन की सरकार में “द्विपक्षीय कन्ट्रोल” शीर्षक के अंतर्गत ईरान के संबंध में अमेरिका की नई नीति लागू हुई। अलबत्ता अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो प्रतिबंध लगा रखा था उसे देश की सीमा से बाहर ले जाने से पहले उसने ईरान के तेल उद्योग के पुनर्निर्माण को लक्ष्य बनाया। इराक द्वारा ईरान पर थोपे गये आठ वर्षीय युद्ध के कारण विभिन्न विशेषकर तेल व गैस के प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंची थी उसके पुनर्निमार्ण में पूंजी निवेश के लिए ईरान ने विदेशी कंपनियों का आह्वान किया। पश्चिमी कंपनियां तेल उद्योग के क्षेत्र में ईरान की संभावनाओं से भलीभांति अवगत थीं इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर ईरान के आह्वान का स्वागत किया। इस मध्य अमेरिका की एक तेल कंपनी को भी ईरान के तेल उद्योग में पूंजी निवेश का मौका मिला।
पश्चिमी कंपनियों विशेषकर एक अमेरिकी कंपनी के ईरान के तेल उद्योग में पूंजी निवेश करने से जायोनी हल्के चिंतित हो गये। ईरान विरोधी जायोनी हल्कों का कहना था कि ईरान-इराक युद्ध से ईरान के तेल प्रतिष्ठानों को जो क्षति पहुंची है उनके पुनरनिर्माण से ईरान दोबारा मज़बूत हो जायेगा। इस बहाने से उन्होंने अमेरिका की तत्कालीन सरकार पर दबाव डाला कि वह अमेरिकी कंपनियों को ईरान में पूंजी निवेश करने से रोके। इन दबावों का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मार्च 1995 में ईरान के तेल उद्योग में अमेरिकी कंपनियों को पूंजी निवेश करने से मना कर दिया। इसके लिए यह बहाना बनाया गया कि ईरान आतंकवाद का समर्थन करता है और वह मध्यपूर्व की तथाकथित शांति वार्ता प्रक्रिया का विरोधी है। चूंकि प्रतीत यह हो रहा था कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने ईरान के तेल उद्योग में अमेरिकी कंपनियों को निवेश करने से जो मना किया था उसका कोई लाभ नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने उसके दो महीने बाद मई 1995 में प्रस्ताव नंबर 12957 को लागू करने का आदेश दिया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत ईरान के साथ समस्त व्यापारिक लेन- देन और ईरान में पूंजी निवेश से मना कर दिया गया। इस फैसले के बाद अमेरिकी तेल कंपनी कानेको Conoco ईरान के तेल बाज़ार में निवेश करने से निकल गयी और तेज़ी से यूरोपीय कंपनियों ने इसका स्थान ले लिया।
यूरोपीय कंपनियों द्वारा ईरान के तेल उद्योग में निवेश करने से ईरान के खिलाफ प्रतिबंध की अमेरिकी नीति विफल हो गयी परंतु अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगा दीं जिसे सेकेन्ड्री प्रतिबंध का नाम दिया गया। ईरान पर प्रतिबंध के संबंध में अमेरिकी कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किये थे उस समय तक उसमें केवल अमेरिकी कंपनियां और नागरिक शामिल थे परंतु क्लिंटन की सरकार के समय से और ईरान व लीबिया के खिलाफ प्रतिबंध के डेमाटो कानून के लागू होने के बाद से तय हुआ कि दूसरे देश और विदेशी कंपनियां भी ईरान के साथ व्यापार नहीं करेंगी और जो देश या विदेशी कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंध की अनदेखी करेंगीं उन पर जुर्माना किया जायेगा। यह एसा विषय था जो देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों से विरोधाभास रखता था। डेमाटो कानून पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अगस्त 1996 में हस्ताक्षर कर दिया। इससे पहले इस कानून को अमेरिकी कांग्रेस और सिनेट में भारी मतों से पारित कर दिया गया था। चूंकि इतालवी मूल के अमेरिकी रिपब्लिकन अलफान्सो डेमाटो को इसका मूल समर्थक समझा जाता था इसलिए यह डेमाटो कानून के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो अमेरिकी या गैर अमेरिकी ईरान के तेल उद्योग में दो करोड़ डालर से अधिक का निवेश करेगा उसे इस कानून में दंडित करने का प्रावधान था। इस बात के दृष्टिगत बहुत सी पश्चिमी कंपनियां ईरान के तेल उद्योग में पूंजी निवेश करने से पीछे हट गयीं। अलबत्ता इसी कानून में अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात की अनुमति दी गयी कि उचित समझने की स्थिति में इस कानून के कुछ उल्लंघन कर्ताओं को दंडित न किया जाये।
इस प्रकार का जो फैसला लिया गया उसका कारण अमेरिका से बाहर प्रतिबंधों पर की जाने वाली प्रतिक्रिया थी। इससे महीनों पहले दूसरे विशेषकर यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी थी कि अगर यह कानून लागू किया और अमेरिका के आंतरिक कानून के आधार पर उनकी कंपनियों को दंडित किया गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे और इसके मुकाबले की कार्यवाही करेंगे। इसी प्रकार इन देशों ने कहा था कि वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अमेरिका की शिकायत करेंगे। यह स्पष्ट व ठोस दृष्टिकोण इस बात का कारण बना कि अमेरिकी अधिकारियों ने सतर्कता की नीति अपनाई और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात की अनुमति दी कि कुछ विदेशी कंपनियों को माफ कर दें। इसी कारण जब फ्रांस की टोटल कंपनी ने ईरान के साथ समझौता किया तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लिखित आदेश में घोषणा की थी कि इस कंपनी को अमेरिका की ओर से दंडित नहीं किया जायेगा। ईरान के साथ फ्रांस की टोटल कंपनी ने जो समझौता किया था उसके मुकाबले में वाइट हाउस के पीछे हट जाने से अमेरिका के इल्सा कानून की अनुपयोगित सामने आ गयी और ईरान के तेल उद्योग में विदेशी कंपनियों के पूंजी निवेश का द्वार खुल गया।
इल्सा कानून की अवधि पांच साल थी। वर्ष 2001 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जार्ड डब्ल्यू बुश की सरकार में इसकी अवधि में वृद्धि कर दी गयी। इसके साथ ही वर्ष 2006 में और एक राजनीतिक परिवर्तन के बाद इस कानून का नाम बदल कर इल्सा 2 रख दिया गया। ज्ञात रहे कि उस समय लीबिया में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन के कारण उसे प्रतिबंधित देशों की सूची से निकाल दिया गया और इल्सा कानून में सुधार किया गया। पहले दो करोड़ डालर तक ईरान के साथ व्यापार करने की अनुमति थी पर अब इसे बढ़ा कर 4 करोड़ डालर कर दिया गया। इसी प्रकार इस कानून की अवधि को बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दिया गया। वर्ष 2016 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इल्सा कानून की अवधि में वृद्धि कर दी। यह वह समय था जब ईरान के साथ परमाणु समझौता हो चुका था। इस आधार पर इस्लामी गणतंत्र ईरान ने अमेरिका के इस क़दम को परमाणु समझौते के खुले उल्लंघन का नाम दिया।
इल्सा कानून बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति काल के दूसरे दौर में और वर्ष 2003 में ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के संबंध में किये जाने वाले हो -हल्ले के आरंभ तक ईरान के खिलाफ अमेरिका की प्रतिबंधों पर आधारित नीति का ध्रुव था। उसी दौर में ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का एक अन्य कानून पारित किया गया। उदाहरण स्वरूप अप्रैल 1996 में “आतंकवाद से मुकाबला और मृत्यु दंड” शीर्षक के अंतर्गत एक कानून पारित किया गया। इसका लक्ष्य ईरान के साथ हर प्रकार के व्यापारिक लेन- देन को रोकना और उन देशों की आर्थिक सहायता को रोकना था जो ईरान को सैन्य संसाधन बेचते थे। इसके बाद अगस्त 1997 में बिल क्लिंटन की सरकार ने भी उन देशों के साथ सहयोग से इंकार कर दिया जो ईरान को सैन्य संसाधन निर्यात करने का इरादा रखते थे। जुलाई 1998 में और उसके बाद जनवरी 1999 में बिल क्लिंटन की सरकार ने 10 रूसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए अमेरिकी सरकार ने बहाना बनाया कि रूसी संस्थाएं ईरान के मिसाइल उद्योग में उसके साथ सहकारिता कर रही थीं। सितंबर 1999 में भी अमेरिकी सरकार ने ईरान में धार्मिक आज़ादी के उल्लंघन के बहाने तेहरान पर नया प्रतिबंध थोप दिया।
अलबत्ता बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति काल के अंतिम समय में और क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय परिवर्तनों से प्रभावित होकर वाइट हाउस ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के दबाव को कम करने की नीति अपनाई। उदाहरण स्वरूप दिसंबर 1998 में अमेरिका ने ईरान का नाम उन देशों की सूची से हटा दिया जिनका नाम मादक पदार्थों के तस्करों की सूची में था। अप्रैल 1999 में भी क्लिंटन ने एक आदेश जारी करके ईरान, लीबिया और सूडान से खाद्य पदार्थों और दवाइयों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया। इसी प्रकार अमेरिकी सरकार ने बोइंग कंपनी को आदेश दिया कि ईरान के यात्री विमानों के लिए जिन कल पुर्ज़ों की खरीदारी हो चुकी है वह उन्हें दे। वर्ष 1953 में एक विद्रोह करवा कर अमेरिका ने ईरान की मोहम्मद मुसद्दिक की कानूनी सरकार को गिरवा दिया था। इसमें वाशिंग्टन की भूमिका व हस्तक्षेप के प्रति मार्च 2000 में अमेरिका की तत्कालीन विदेशमंत्री मैडलिन आलब्राइट ने एक भाषण में खेद जताया और उसके बाद क़ालीन, केवियर और पिस्ता जैसी गैर पेट्रोलियम चीजों के अमेरिका निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा था उसे समाप्त कर दिया गया। इन सबके बावजूद अमेरिका में सरकार के बदलने और जार्ज डब्ल्यू बुश के सत्ता में आने से ईरान के खिलाफ शत्रुता पर आधारित नीति को गति मिली।