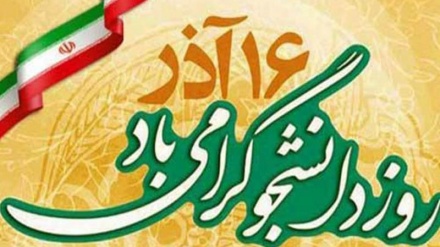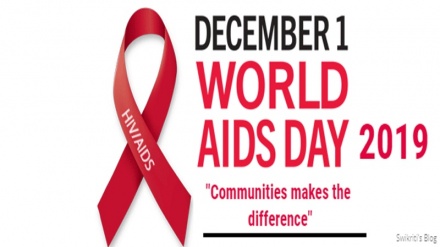ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी प्रतिबंध- 3
आपको याद होगा कि पिछली दो कड़ी में हमने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी सरकार की पाबंदी लगाने की नीति के व्यवहारिक होने के क्रम, तेहरान में अमरीकी दूतावास पर नियंत्रण की घटना के आधार पर ईरान के ख़िलाफ़ आरंभिक पाबंदियां और ईरान पर आतंकवाद का समर्थन, मानवाधिकार के उल्लंघन और मध्यपूर्व में कथित शांति प्रक्रिया का विरोध करने जैसे इल्ज़ाम पर चर्चा की।
इसी तरह हमने बताया कि कुवैत के अतिग्रहण की घटना में इराक़ की हार के बाद तत्कालीन अमरीकी सरकार ने ईरान से मुक़ाबले के लिए ‘द्विपक्षीय नियंत्रण’ की नीति अपनायी और सेकेन्ड्री पाबंदियों के नाम से नई पाबंदियां लगाई गई। इन पाबंदियों के आधार पर हर कंपनी पर चाहे वह अमरीकी हो या ग़ैर अमरीकी, ईरान के पेट्रोलिमय उद्योग में पूंजि निवेश करने की स्थिति में जुर्माना लगता। यह ऐसा फ़ैसला था जिसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर योरोपीय संघ में वॉशिंग्टन के व्यापारिक भागीदारियों ने आवाज़ उठायी।
यह घटन उस समय शुरु हुयी जब अमरीकियों ने इराक़ पर दुबारा हमले और सद्दाम के पतन के बाद क्षेत्र में ग्रेटर मिडिल ईस्ट की साज़िश को व्यवहारिक बनाने की कोशिश की। लेकिन यह साज़िश ईरान को झुकाए बिना मुमकिन न थी। इसी वजह से नई साज़िश रची गयी जिसके तहत ईरान को क्षेत्र को अशांत करने वाला देश दर्शाने की कोशिश की गयी बल्कि इससे भी आगे ईरान को विश्व शांति के लिए ख़तरा दर्शाने की कोशिश की गयी। इस साज़िश को व्यवहारिक करने के लिए अमरीकियों ने एमकेओ नामक आतंकवादी गुट को इस्तेमाल किया जिसने यह दावा किया कि ईरान नतन्ज़ में अपने गुप्त प्रतिष्ठान में परमाणु हथियार बनाने का इरादा रखता है। ईरान की ओर से इस दावे को कड़ाई से रद्द किए जाने के बावजूद पश्चिम का प्रचारिक तंत्र ईरान के ख़िलाफ़ दूषित माहौल बनाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदी पर आधारित प्रस्तावों को पारित कराने में सफल हो गया। परमाणु मामले से पहले तक अमरीका की ओर से लगायी गयी पाबंदियों का उसके कुछ निकटवर्ती राजनैतिक व आर्थिक घटक ही समर्थन करते थे लेकिन परमाणु मामले के दुष्प्रचार के बाद यह पाबंदियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो गयीं।
हालांकि इससे पहले इस्लामी गणतंत्र ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण होने को साबित करने के लिए योरोप के तीन देशों जर्मनी, ब्रिटेन और फ़्रांस के साथ इस बात पर सहमत हुआ कि वह परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के पूरक प्रोटोकॉल को अपनी मर्ज़ी से लागू करने के लिए तय्यार है। ऐसा लग रहा था कि यह नीति तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लयू बुश के दुष्प्रचार के असर को ख़त्म कर देगी। लेकिन चूंकि अमरीकी अपनी अस्ल साज़िश यानी ग्रेटर मिडिल ईस्ट की योजना को लागू करने के लिए ईरान को झुकाने में लगे थे, ईरान और तीन योरोपीय देशों के बीच हुयी परमाणु सहमति को जो सादाबाद सहमति के नाम से मशहूर है, रद्द कर दिया। अमरीका की ओर से रुकावट के कारण योरोपीय संघ में ईरान के साथ वार्ता करने वाले पक्ष भी अपने वचन पर पालन करने से पीछे हट गए। अब तेहरान के पास अपने परमाणु अधिकार की प्राप्ति के लिए सेन्ट्रीफ़्यूज को चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसे परमाणु ईंधन की ज़रूरत थी। ईरान के इस फ़ैसले को पश्चिम ने बहाना बनाया और 2006 में ईरान के परमाणु मामले को वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए के कार्यालय से न्यूयॉर्क पहुंचा दिया ताकि ईरान के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पारित कराए। 2006 में ईरान के परमाणु मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचने से लेकर 2013 में जनेवा में ईरान और गुट पांच धन एक के बीच अस्थायी सहमति की प्राप्ति तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के ख़िलाफ़ 6 प्रस्ताव पारित हुए। यह छह प्रस्ताव इस तरह हैं, 2006 में प्रस्ताव नंबर 1696, 2006 में प्रस्ताव नंबर 1737, 2007 में प्रस्ताव नंबर 1747, 2008 में प्रस्ताव नंबर 1803, 2008 में प्रस्ताव नंबर 1835 और फिर अंत में 2010 में प्रस्ताव नंबर 1929। ये सभी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के सातवें अनुच्छेद के तहत पारित हुए कि इस अनुच्छेद में सदस्य देशों को इस बात की इजाज़त दी गयी है कि वे विश्व शांति व सुरक्षा के लिए ख़तरे का मुक़ाबला करने के बहाने ग़लती करने वाले सदस्य देशों के ख़िलाफ़ आर्थिक पाबंदियों सहित व्यवहारिक क़दम उठाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के ख़िलाफ़ तीसरे प्रस्ताव के पारित होने के बाद ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियां लागू होने लगीं। शुरु में ईरान की परमाणु गतिविधियों और इससे जुड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगायी गयीं लेकिन धीरे-धीरे अमरीकियों ने पाबंदियों के इस दायरे को ईरान की अर्थव्यवस्था के दूसरे भाग, बैंको, बीमा कंपनियों, परिवहन कंपनियों और ईरान के तेल की बिक्री तक फैला दिया। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पाबंदियों में खाद्य पदार्थ और दवाओं को अपवाद रखा गया था वे भी इन पाबंदियों से प्रभावित हुए क्योंकि विदेशी बैंक ईरान के साथ मामला करने से दामन बचाने लगे। अमरीकियों ने इन पाबंदियों को मानव इतिहास में सबसे व्यापक पाबंदी का नाम दिया और तत्कालीन अमरीकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों को स्मार्ट पाबंदी बताते हुए कहा था कि इन कार्यवाहियों से ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी।
ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों के बढ़ते दायरे के साथ साथ ईरान का शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम भी विकसित होता रहा यहां तक कि पाबंदियों से पहले तक सेन्ट्रीफ़्यूज की तादाद 1000 से कम थीं वे पाबंदियों के बाद 20000 तक पहुंच गयीं। इसके साथ ही ईरान ने तेहरान के अनुसंधानिक रिएक्टर और रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के लिए ज़रूरी ईंधन के उत्पादन के चरण को भी पूरा करते हुए 20 फ़ीसद युरेनियम का संवर्धन कर दिखाया। इस क़दम से ईरान ने यह दर्शा दिया कि वह अमरीका की अगुवाई में पश्चिम की पाबंदी लगाने की नीति का डटकर मुक़ाबला करेगा। इस सैद्धांतिक नीति के अपनाने के बाद अमरीकियों ने ईरान पर दबाव बढ़ा दिया। अलबत्ता उन्होंने अपने व्यवहार का औचित्य पेश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का सहारा लिया। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के ख़िलाफ़ दुनिया के देशों को अपने साथ मिलाने में अमरीकी दबाव किस हद तक प्रभावी रहा।
मिसाल के तौर पर अमरीका ने दुनिया के सभी देशों को ऐसे दोराहे पर पहुंचा दिया कि वे ईरान के साथ आर्थिक व व्यापारिक संबंध को ख़त्म करें या फिर अमरीका के वित्तीय सिस्टम से बाहर निकलने का ख़तरा मोल लें। इस व्यवहार के कारण बहुत से देश और विदेशी कंपनियों ने अमरीकियों की ओर से दंडित होने के डर से ईरान के मुनाफ़ा देने वाले बाज़ार को छोड़ने का फ़ैसला किया। इस बीच कुछ एशियाई देशों के लिए जिन्हें ईरान से तेल ख़रीदने की इजाज़त थी, यह ज़रूरी हो गया कि वे हर छह महीने में ईरान से तेल आयात की अपनी मात्रा में कमी लाएं ताकि ईरान का तेल निर्यात शून्य पर पहुंच जाए।
इसी तरह अमरीकियों ने ईरान के केन्द्रीय बैंक और ईरानी मुद्रा रियाल में लेन-देन पर पाबंदी लगा कर जो दुनिया के आर्थिक इतिहास में अभूतपूर्ण क़दम था, तेल के निर्यात से हासिल होने वाली विदेशी मुद्रा तक ईरान की पहुंच को रोक दिया। अमरीकियों के इस क़दम के बाद योरोपीय संघ ने भी यूरो में ईरान के साथ मामले करने से मना कर दिया और स्वीफ़्ट तंत्र पर उसकी पहुंच पर रोक लगा दी।
एक ओर अमरीकी विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चरणबद्ध रूप में प्रस्ताव पारित करवा कर उसे लागू कर रहे थे तो दूसरी ओर इसी के साथ देश के भीतर भी ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबंदियों के बिल पास कर रहे थे। मिसाल के तौर पर जुलाई 2010 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने “ईरान में पूंजी निवेश पर रोक ओर व्यापाक पाबंदी क़ानून” नामक बिल पर दस्तख़त किए कि जिसके आधार पर ईल्सा नामक क़ानून के तहत पड़ने वाला दबाव बढ़ता और परमाणु गतिविधियां और देश से बाहर तेल की ख़रीदारी पर असर पड़ता। ईल्सा नामक क़ानून 1996 में ईरान और लीबिया के ख़िलाफ़ पारित हुआ था। अमरीकियों को लगा कि ईरान के तेल के निर्यात और इस देश के केन्द्रीय बैंक पर पाबंदी के बाद, तेल की बिक्री पर रोक लगाकर इस्लामी गणतंत्र ईरान पर पहले से ज़्यादा दबाव बढ़ा देंगे।
इस बीच अमरीका की ओर से ग़ैर आर्थिक पाबंदियां लगीं जिनसे स्पष्ट होता जा रहा था कि अमरीका ईरान के परमाणु कारय्कर्म को रुकवाने के लिए किसी भी तरह की कार्यवाही से नहीं हिचकिचाएगा। 2006 में अमरीका में एक फ़ेडरल अदालत ने आदेश दिया कि ईरान की तख़्त जमशीद नामक पुरातात्विक धरोहर को ज़ायोनी शासन के हित में छीन लिया जाए। यह दुनिया की सबसे बड़ी धरोहरों में एक है। उधर अमरीका की माइक्रोसॉफ़्ट और याहू कंपनियों ने अमरीकी सरकार के दबाव में एलान किया कि वे ईरान का नाम उस लिस्ट से निकाल देंगी जिन देशों को इंटरनेट सेवा दी जाती है लेकिन यह क़दम भी ईरानी राष्ट्र व सरकार को अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के दायरे में अपने परमाणु अधिकार से लाभ उठाने के संकल्प से न रोक सका। यही वजह है कि अंत में पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामी गणतंत्र ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पत्राचार और ईरान के परमाणु अधिकार को मान्यता देने के वचन के ज़रिए विगत के व्यवहार में सुधार किया और इस तरह परमाणु सहमति तक पहुंचने का रास्ता समतल हुआ। जनेवा में होने वाली बातचीत में ईरान और गुट पांच धन एक इस बात पर सहमत हुए कि अंतिम सहमति तक पहुचने से पहले ईरान की ओर से परमाणु कार्यक्रम को अस्थायी तौर पर रोकने के बदले में अमरीका और उसके घटक ईरान के ख़िलाफ़ सुरक्षा परिषद में नया प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे।