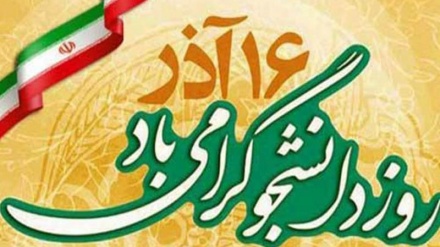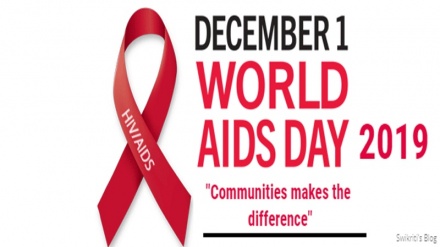प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था-2
देशों के आर्थिक विकास की नीतियों की समीक्षा से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था और घरेलू उत्पाद को मज़बूत बनाना उन आवश्यक बातों में से है जिन्हें कुछ प्रगतिशील देशों ने व्यवहारिक बनाया है और उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं।
उदाहरण स्वरूप भारत और ब्राज़ील जैसी दो उभरती हुई आर्थिक शक्तियों ने 70 के दशक के बाद से घरेलू उत्पाद को मज़बूत बनाने और विदेशी झटकों के मुक़ाबले में अपनी अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाले नुक़सान को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक आयात की रणनीति का अनुसरण किया। इसका अर्थ यह है कि जिन देशों में कुछ वस्तुओं के उपभोग की आंतरिक मंडी बहुत बड़ी है वे इन वस्तुओं के आयात के बजाए उनका घरेलू उत्पादन शुरू कर दें ताकि इस तरह घरेलू पैदावार को मज़बूत बना कर और रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करके अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना दिया जाए।
यद्यपि इन नीतियों के ब्राज़ील के सौ अरब डॉलर से अधिक के क़र्ज़ों जैसे कुपरिणाम भी सामने आए हैं लेकिन ब्राज़ील ने अर्थव्यवस्था के मुख्य मानकों को बेहतर और घरेलू उद्योगों को मज़बूत बना कर यह दर्शा दिया कि वर्तमान संसार की उभरती हुई आर्थिक शक्ति बना जा सकता है। भारत ने भी इसी तरह की नीति अपना कर और देसी उत्पादों को मज़बूत बना कर तथा सौ करोड़ से अधिक की मंडी से लाभ उठा कर अपने आपको संसार की उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में पेश करने में सफलता पाई है।
चीन ने भी 1949 में माओ क्रांति के बाद आरंभ में देश के भीतर कृषि विकास की रणनीति पर काम किया और कृषि के क्षेत्र को मज़बूत बनाने के साथ ही लघु उद्योगों की सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित किया। चीन ने उत्पादन की क्षमता बढ़ाने और इसी तरह अपने राजनैतिक प्रभुत्व को मज़बूत बनाने के लिए 1966 में सांस्कृतिक क्रांति आरंभ की और अंततः 1977 में डेंग शियावपिंग के 1977 में सत्तासीन होने के बाद इस देश में नए परिवर्तन शुरू हो गए जिनसे चीन में ध्यान योग्य आर्थिक प्रगति हुई। चीन वर्ष 2002 में विश्व व्यापार संगठन से जुड़ गया और इसके बाद अधिक आर्थिक सुधारों के साथ चीन की आर्थिक प्रगति में और भी गति आ गई।
जापान और फ़्रान्स ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अपने आर्थिक और औद्योगिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के आयात को अत्यधिक सीमित कर दिया। कुछ ही बरसों में इस नीति और घरेलू उत्पादन के समर्थन के चलते यह दोनों देश, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मैदान के दो अहम खिलाड़ी बन गए। अलबत्ता कुछ समय के बाद इन दोनों देशों ने प्रतिस्पर्धक व स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के मार्ग पर क़दम बढ़ाते हुए आयात की सीमितता को ख़त्म कर दिया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यद्यपि अन्य देशों ने प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया है लेकिन वे भी कुछ ख़ास नीतियां अपना कर विदेशी झटकों के मुक़ाबले में अपनी अर्थव्यवस्था और घरेलू उत्पाद को मज़बूत बनाने जैसे लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयास में रहे हैं।
इस प्रकार के क़दम उठाए जाने के दीर्घगामी प्रभाव होते हैं जिनका परिणाम कठिन परिस्थितियों को सहन करने और प्रतिबंधों या अचानक पड़ने वाले आर्थिक और वित्तीय झटकों जैसे दबाव के सामने डटे रहने की क्षमता पैदा होने के रूप में निकलता है। विश्व स्तर पर आर्थिक प्रतिबंधों के इतिहास पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालने से पता चलता है कि पहले विश्व युद्ध से लेकर 1990 तक विभिन्न देशों के ख़िलाफ़ 115 बार आर्थिक प्रतिबंध पारित और लागू हुए हैं। इनमें से 77 मामलों अर्थात 67 प्रतिशत प्रतिबंधों का संबंध अमरीकी सरकार से है जो उसने 1918 से 1990 के बीच लगाए हैं। 1990 में पूर्व सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आर्थिक प्रतिबंध के हथकंडे के तोर पर इस्तेमाल में अमरीका सबसे आगे रहा। इस प्रकार से कि 1990 से 1999 के वर्षों में पूरे संसार के आर्थिक प्रतिबंधों का 90 प्रतिशत भाग अमरीका से विशेष रहा। केवल बिल क्लिंटन के पहले राष्ट्रपतित्व काल में ही अमरीकी सरकार ने संसार की 2.3 अरब जनसंख्या वाले या दूसरे शब्दों में संसार की कुल जनसंख्या का 42 प्रतिशत भाग रखने वाले 35 देशों पर 61 बार आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इस प्रकार की कठिन आर्थिक परिस्थितियों से मुक़ाबले में आर्थिक सुरक्षा या दूसरे शब्दों में प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा बरागर हो सकती है।
झटकों और दबाव के मुक़ाबले में आर्थिक सुरक्षा, मज़बूत अर्थव्यवस्था के अनेक मानकों पर निर्भर होती है। इन मानकों में स्वदेश निर्मित वस्तुओं
इस आधार पर प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था की दिशा, प्रगति की रुकावटों को दूर करने और प्रगति व विकास के मार्ग में प्रयास की ओर होती है। इस दृष्टि से प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था और आर्थिक मितव्ययिता में काफ़ी अंतर है क्योंकि प्रतिरोधक अर्थव्यवस्था में स्रोतों की सीमितता नहीं होती लेकिन मौजूद स्रोतों से उचित ढंग से लाभ उठाने की प्रक्रिया एक निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत होती है। यह ऐसी स्थिति में है कि जब आर्थिक मितव्ययिता में लोगों को स्रोतों और पूंजी की सीमितता का सामना करना पड़ता है, सभी के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है और कम उपभोग के माध्यम से सीमितताओं का मुक़ाबला किया जाता है।
भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में मूल रूप से जिन देशों की उचित आर्थिक स्थिति नहीं होती वे बाहरी आर्थिक शक्तियों के मुक़ाबले में बहुत नुक़सान उठाते हैं। यह स्थिति, लोगों में अप्रसन्नता, मुद्रा स्फ़ीति, बेरोज़गारी और मंदी का कारण बनती है और एक ख़तरे में परिवर्तित हो जाती है। कुछ अर्थ शास्त्रियों के विचार में आर्थिक सुरक्षा की दर को बढ़ाने में एक प्रभावी शैली, क्षेत्रीय आर्थिक समरसता को सुदृढ़ बनाना है।
हमेशा से संसार में क्षेत्रीय सहयोग का रुझान पाया जाता रहा है लेकिन वैश्विक परिवर्तनों की प्रक्रिया विशेष कर दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति ने इस रुझान में वृद्धि पैदा कर दी। यह सहयोग विभिन्न रूपों में और अलग-अलग स्तरों पर सभी राजनैतिक, आर्थिक, सुरक्षा व सामाजिक मैदानों में शुरू हुए हैं। यद्यपि दूसरे विश्व युद्ध के बाद का अनुभव नैटो जैसी क्षेत्रीय संधियों और समझौते के गठन में पूरब व पश्चिम के राजनैतिक प्रभाव को दर्शाती हैं लेकिन समय बीतने और सोवियत संघ के विघटन जैसे परिवर्तनों के कारण राजनैतिक हित धीरे-धीरे क्षेत्रीय संगठनों से विलुप्त होने लगे और आर्थिक विकास ने उनका स्थान ले लिया।
अर्थ शास्त्रियों का मानना है कि क्षेत्रीय आर्थिक समरसता जैसी बातें बड़ी हद तक उन वित्तीय संकटों और आर्थिक मंदी के कुपरिणामों को कम कर सकती हैं जिन्हें वर्ष 1997 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में देखा गया था। इस आधार पर दक्षिणी अमरीका जैसे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मोर्कोसोर और अल्बता जैसे संगठन बना कर आर्थिक समरसता की ओर देशों का रुझान अधिक मज़बूत हुआ है। आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय सहकारिता का सबसे अहम रूप है जो देशों की आंतरिक अर्थव्यवस्था के ढांचे को मज़बूत बनाने में सहायता करता है क्योंकि संसार के किसी भी देश के पास अकेले ही उत्पादन के सभी स्रोत और साधन नहीं होते और सभी को इस संबंध में सीमितता का सामना होता है। दूसरी ओर आर्थिक सहयोग, धन, शक्ति और संपन्नता का भी कारण बनता है और राजनैतिक व सुरक्षा संबंधी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकारों की सहायता करता है। आर्थिक समरसता, क्षेत्र से बाहर की शक्तियों पर निर्भरता को कम करने में भी सहायक है और क्षेत्रीय सुरक्षा का कारण बनती है।
कुल मिला कर यह कहा जाना चाहिए कि आर्थिक ख़तरे भी सैन्य ख़तरों की तरह देशों व सरकारों पर प्रभाव डालते हैं और आर्थिक समस्याओं की जटिलता और देशों की आर्थिक कमज़ोरी के अनुपात में ही वे देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को लक्ष्य बनाते हैं। इस आधार पर आर्थिक सुरक्षा, अचानक लगने वाले झटकों के मुक़ाबले में अर्थव्यवस्था की मज़बूती, किसी भी कारण वस्तुओं की कमी से पैदा होने वाले दबाव जैसे कड़े हालात में लचक और आगे की ओर बढ़ने वाली और स्थानीय विज्ञान पर निर्भर अर्थव्यवस्था जैसी तीन पर आधारित होती है और इन्हीं तीन बातों को आर्थिक सुरक्षा का आधार कहा जा सकता है।